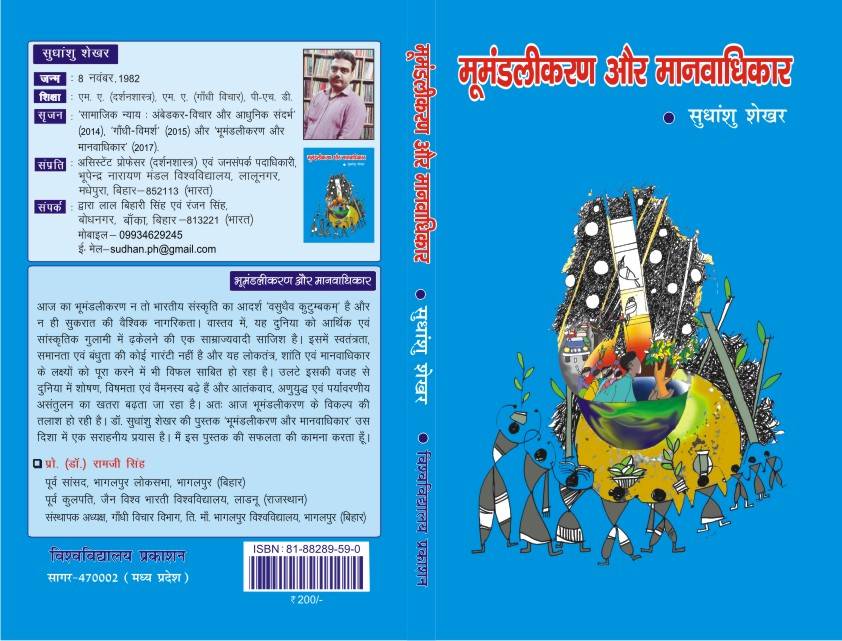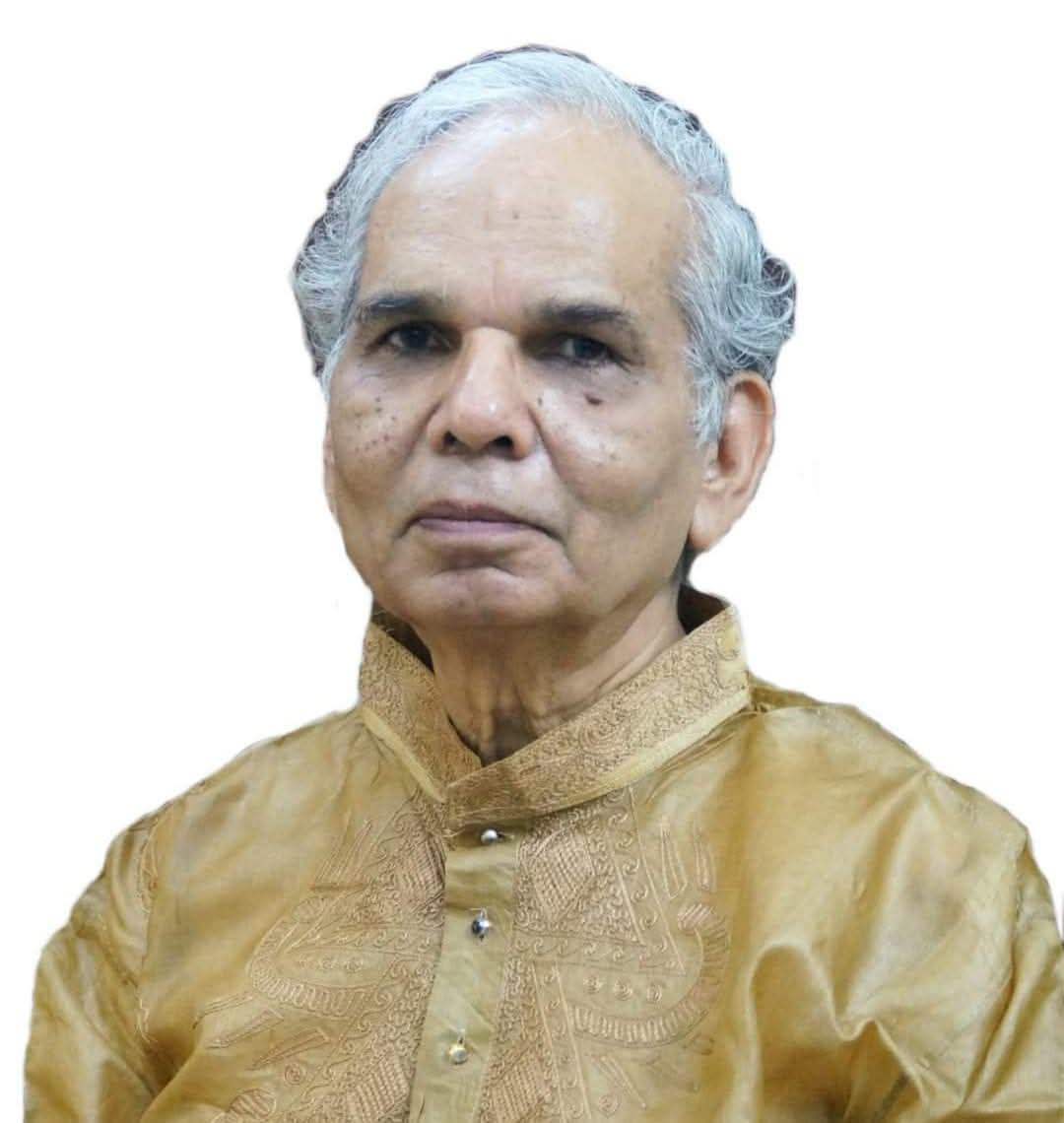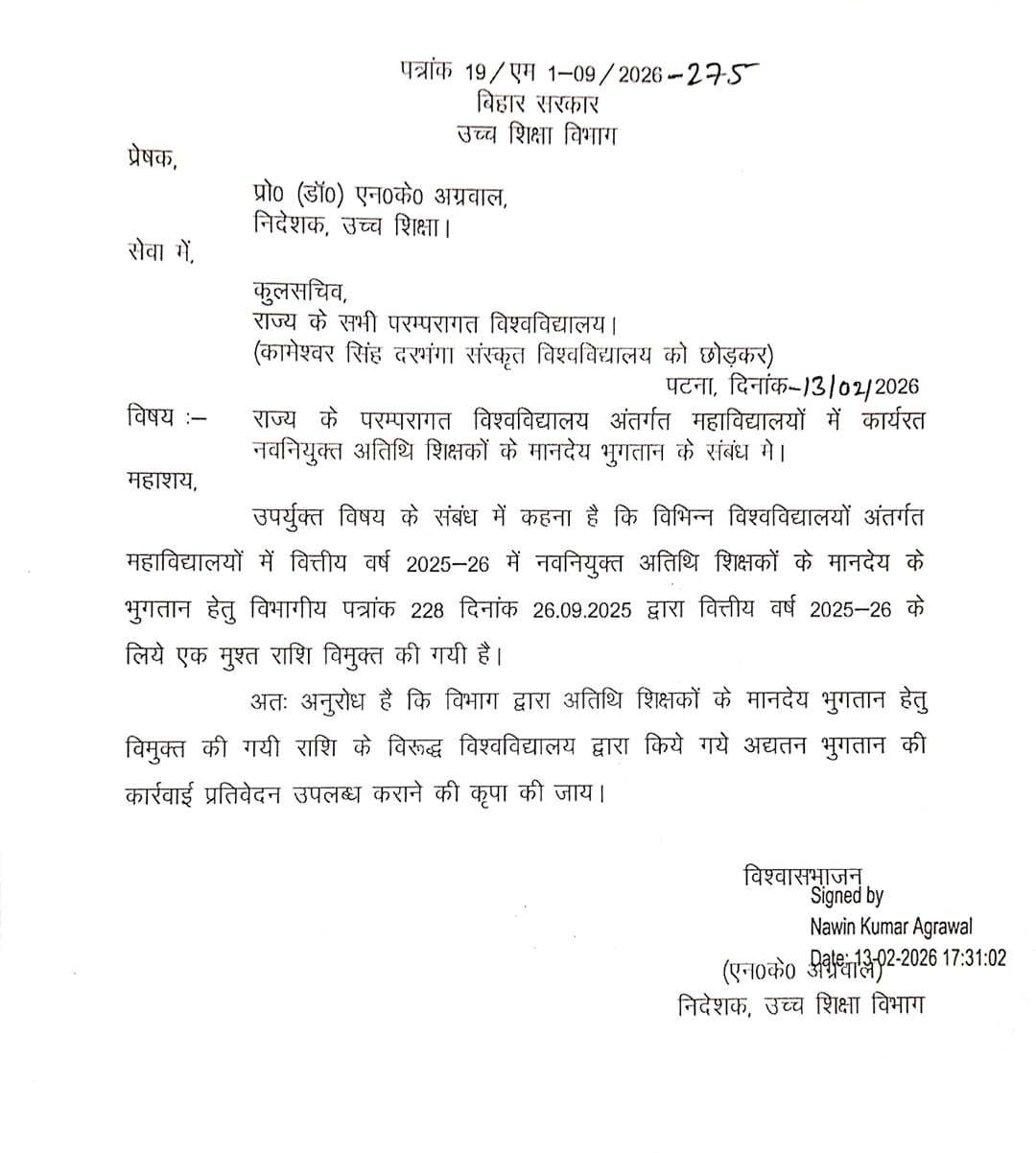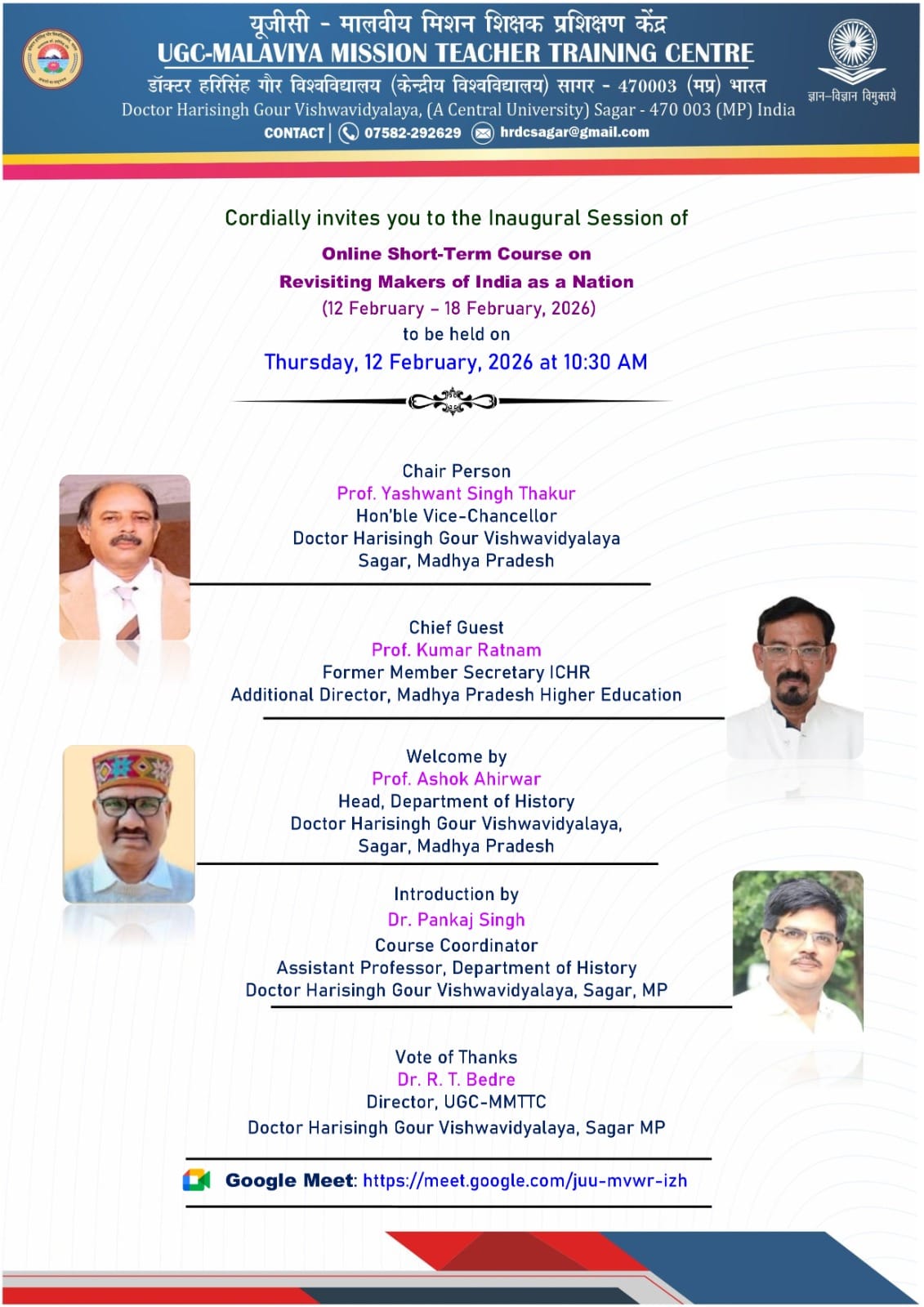7. भूमंडलीकरण और पर्यावरण
प्रकृति-पर्यावरण1 के संरक्षण एवं संवर्द्धन को ध्यान में रखकर भारतीय दार्शनिकों ने न केवल मनुष्य, बल्कि समस्त जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, प्रकृति-पर्यावरण आदि के बीच मानव जीवन की समरसता, सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित करने वाली जीवन-दृष्टि विकसित की थी।2 भारतीय मनीषियों का संपूर्ण जीवन और दर्शन पर्यावरणीय नैतिकता का पोषक है।3 आवश्यकताओं में कटौती, लोभ-लालच का त्याग, अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप, कुटीर उद्योग, स्वावलम्बन, सर्वोदय आदि के बारे में उनके विचार तथा प्रकृति के प्रति उनका असीम लगावऋ ये सभी उनकी सूक्ष्म पर्यावरण-चेतना की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रमपूर्वक अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए और उसी से संतोषपूर्वक जीवनयापन करना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि आवश्यकताओं में कटौती करके श्रम द्वारा अर्जित धन से ही मनुष्य सुख, संतोष एवं शांति की प्राप्ति कर सकता है और एक सच्चा एवं जीने योग्य जीवन जी सकता है। महात्मा गाँधी का भी कहना है कि प्रकृति के पास मनुष्य को देने के लिए बहुत कुछ है, वह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन वह उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा है, ”मनुष्य की वृत्तियाँ चंचल हैं। उनका मन बेकार की दौड़-धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे-जैसे ज्यादा दिया जाय वैसे-वैसे ज्यादा माँगता है। ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बाँध दी।“4
जाहिर है कि ‘सादा जीवन और उच्च विचार’ ही प्राकृतिक जीवनशैली का सूत्रा है। जैसा कि गाँधी ने लिखा है, ”बहुत सोचकर उन्होंने (हमारे पुरखों ने) देखा कि सुख-दुःख तो मन के कारण हैं। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे। ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई।“5 अपनी कालजयी पुस्तक ‘हिंद-स्वराज’ में महात्मा गाँधी ने जिस समाज-व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसमें पर्यावरण संरक्षण और नैतिकता के तत्व भरे पड़े हैं। गाँधी कहते हैं, ”सभ्यता वह आचरण है, जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है, फर्ज अदा करने का अर्थ है, नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को (अपने असली स्वरूप को) पहचानते हैं। यही सभ्यता है।“6 जाहिर है कि सच्ची सभ्यता की गाँधीय अवधारणा में नीति की बात शामिल है, जो कि पर्यावरण-संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हुए गाँधी ने लिखा, ”शरीर को सुख कैसे मिले, यही आज की सभ्यता ढूँढती है, और यही देने की कोशिश करती है। परन्तु वह सुख भी नहीं मिल पाता। यह सभ्यता तो अधर्म है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धरकर बैठे रहेंगे, तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। पैगम्बर मुहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म उसे निरा ‘कलजुग’ कहता है। यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद भी नाशवान है।“7 इसलिए, उन्होंने लोगों को बराबर इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अनावश्यक रूप से धन का संचय न करें और यदि उनके पास आवश्यकता से अधिक धन हो, तो इसके ट्रस्टी बन जाए और समाज के निर्धन एवं अभावग्रस्त समुदाय के हित में इसे खर्च करें। अगर, अपरिग्रह एवं ट्रस्टीशिप को हम अपने व्यवहार में लाएँ, तो प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने एवं उसका संचय करने की होड़ लगी रहती है, परन्तु गाँधी ने आवश्यकता से अधिक धन-अर्जन और धन⪅ को चोरी की संज्ञा दी थी। उन्होंने लिखा है, ”जो अर्थशास्त्रा धन की पूजा करना सिखाता है और बलवानों को दुर्बलों का शोषण करनके धन-संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्रा का नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो एक झूठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अपनाकर हम मृत्यु को न्यौता देंगे।“8
गाँधी बड़े-बड़े कारखानों में विपुल मात्रा में माल पैदा करने की बजाय देश के विशाल जनसमुदाओं द्वारा अपने घरों और झोपड़ों में माल का उत्पादन करने के हिमायती थे।9 गाँधी ने कुटीर उद्योग एवं स्वावलंबन पर जोर दिया था। कुटीर उद्योग जहाँ एक ओर स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं, वहीं वे नाम मात्रा प्रदूषण पैदा करते हैं। कुटीर उद्योगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन रूक जाएगा और इन संसाधनों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह सर्वविदित है कि बड़े-बड़े कल-कारखाने और बृहत् पैमाने पर उत्पादन हेतु बड़े-बड़े उद्योग आज जितना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और फैला रहे हैं, उससे पर्यावरण को भयानक रूप से क्षति हो रही है। गाँधी के शब्दों में, ”बड़े पैमाने पर होने वाला सामूहिक उत्पादन ही दुनिया की मौजूदा संकटमय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। एक क्षण के लिए यदि मान भी लिया जाए कि यंत्रा मानव-समाज की सारी आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं, तो भी उसका यह परिणाम तो होगा ही कि उत्पादन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हो जाएगा और वितरण की योजना के लिए हमें द्रविड़ी प्राणायाम करना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि जिन क्षेत्रों में वस्तुओं की आवश्यकता है, वहीं उनका उत्पादन और वहीं वितरण हो, तो वितरण का नियंत्राण अपने आप हो जाता है। जब उत्पादन और उपभोग दोनों स्थानीय बन जाते हैं, तब अनिश्चित मात्रा में और किसी भी मूल्य पर उत्पादन की गति बढ़ाना बंद हो जाता है।“10
हम जानते हैं कि आधुनिक सभ्यता और उसके यंत्रा-तंत्रा ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है।11 इसकी अदूरदर्शी अनीतियों के कारण प्राकृतिक संपदाएँ नष्ट हो रही हैं और पर्यावरण-असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यंत्रा संबंधी गाँधी के विचारों की ओर हमारा ध्यान जाना स्वभाविक है। गाँधी औद्योगिक सभ्यता के मूलाधार बड़े-बड़े कल-कारखाने और मनुष्यों को बेरोजगार करने वाले यंत्रों के विरोधी थे। उनके शब्दों में, ”यंत्रा आधुनिक सभ्यता की मुख्य निशानी है और वह महापाप है। … यंत्रा तो साँप का ऐसा बिल है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों साँप होते हैं। एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहाँ यंत्रा होंगे, वहाँ बड़े शहर होंगे। जहाँ बड़े शहर होंगे, वहाँ ट्रामगाड़ी और रेलगाड़ी होगी। वहीं बिजली की बत्ती की जरूरत रहती है। … यंत्रा का गुण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जबकि उसके अवगुणों पर मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ।“12 आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार सारे अत्याधुनिक यंत्रा साम्राज्यवादियों एवं पूंजीवादियों के नियंत्राण में चले गए हैं। डाॅ. सरोज कुमार वर्मा लिखते हैं, ”गाँधी यंत्रा को लोगों के शोषण और गुलामी के औजार के रूप में देखते थे, इसलिए उसका विरोध करते थे। परन्तु जब उन्हें लगा कि यह शरीर भी यंत्रा है और चरखा भी, दाँत कुरेदने वाली सीकी भी यंत्रा है और कपड़ा सीने वाली सूई भी ऐसे यंत्रों के बगैर जीवन संभव नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपना विरोध कम किया।“13 फिर गाँधी ने कहा है ”मेरा विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है, उसके लिए है। … मेरा उद्देश्य तमाम यंत्रों का नाश करने का नहीं है, बल्कि उनकी हद बाँधने का है।“14
वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण प्रदूषण की समस्या मुख्यतः मनुष्य के अनियंत्रित भोग-विलास एवं अनैतिक जीवन-पद्धति का ही परिणाम है। विकास की चकाचैंध में मनुष्य प्रकृति-पर्यावरण से अपना प्रेमपूर्ण संबंध बिगाड़ चुका है और अपनी तबाही की राह बना रहा है। जगह-जगह बाढ़-सुखाड़, भूकंप, सुनामी एवं अम्लवृष्टि का संकट छा गया है। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ एवं ‘ग्लोबल कूलिंग’ और ओजोन की छतरियों के क्षरण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। धरती अपनी ऊर्वरा शक्ति खो रही है, पेयजल संकट गंभीर रूप धारण कर चुका है और ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में सांस लेने के लिए शुद्ध आॅक्सिजन मिलना भी मुश्किल है। भविष्य के मानव के बारे में कहा जा रहा है, ”यह कंक्रीट के जंगल में पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए अम्लरोधक तथा विशेष रसायनयुक्त प्लास्टिक के कपड़ों से अपने शरीर को ढंककर चलेगा और पीठ पर आॅक्सीजन का सिलिंडर लादे, कंधे पर पानी की बोतल लटकाए, नाक में गैस मास्क लगाए तथा कान में ध्वनि अवरोधक यंत्रा कसे औद्योगिक विकास का कवच ढोएगा।“15
निष्कर्ष : भूमंडलीकरण का तथाकथित विकास अभियान, वास्तव में संपूर्ण मानवता के लिए महाविनाश की आख्यान बनने वाला है। ऐसे में दुनिया भर में इस शैतानी (आधुनिक) सभ्यता के विकल्प की तलाश हो रही है और इस क्रम में जगह-जगह पर्यावरण-संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। ‘विकास और पर्यावरण’ जैसे विषय पर काफी गंभीरता से विचार-विमर्श हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण-संरक्षण का प्रश्न पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिणऋ सभी के समान हित का प्रश्न है। आज दुनिया के अधिकांश चिंतक और वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि विकास का वर्तमान रास्ता विनाश की ओर ले जाने वाला है। मौजूदा औद्योगिक ढाँचे को चलाने वाले लोग भी प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण और पर्यावरण-संतुलन की बात करने लगे हैं, भले ही उनके काम इस भावना के विपरीत पड़ते हों।16
भूमंडलीकरण के कर्ताधर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय संकटों के समाधान के लिए किए जा रहे ढोंग में भारत भी साथ दे रहा है। जबकि, आज यह साबित हो चुका है कि आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था एवं उसके मूल्यों को बदले बगैर इसके दुष्परिणामों से बचना असंभव है। इस बाबत सुनील कुमार लिखते हैं, ‘‘मानव सभ्यता पर आए इन संकटों का समाधान इस व्यवस्था में नहीं हो सकता। हम छोटे-छोटे उपाय आजमाकर उससे स्थायी हल चाहते हैं! जैसे कि कार्बन-डाय-आॅक्साइड की मात्रा कम करने की जरूरत है। तो इसके लिए जीवनशैली को बदलने और औद्योगीकरण कम करने के बजाय विकसित देशों ने एक रास्ता निकाल लिया कि वे खुद तो यह गैस छोड़ते रहेंगे और इसके बदले पैसे दे देंगे, जबकि विकासशील देश पर्यावरण सुधारेंगे, जंगल लगाएंगे! तो यह हुआ वैश्विक रूप से एक विकट समस्या का एक बाजारू हल!! … लेकिन ऐसे हलों से संकट खत्म नहीं होेंगे।“ इस संबंध में समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा लिखते हैं, ‘‘इस युग (गाँधी-युग) के साथ अलग तरह की विश्व-दृष्टि जुड़ी है। इसमें मनुष्य की नियति प्रकृति या वनस्पति जगत सहित अन्य प्राणियों पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनके साथ एक नए तरह का तादात्म्य स्थापित करना है। आज पर्यावरण की सुरक्षा, जो अन्य जीवों और वनों की रक्षा से जुड़ा है, मानव प्रजाति के स्वयं जीवित रहने की अनिवार्य शर्त दिखाई देने लगी है। ऐसे में पर्यावरण-संतुलन को बनाए रखने के लिए विकास के लक्ष्य को बिलकुल बदल देना जरूरी है।“17
जाहिर है कि भारतीय दर्शन के अपनाकर ही मनुष्य एवं मानवता का भला हो सकता है। अतः, अब हमें बिना समय गंवाए भारतीय विचारों के आलोक में पर्यावरण के साथ मैत्राी वाला विकास (‘इकोफ्रेंडली डेवलपमेंट’), टिकाऊ विकास (‘स्सटनेबुल डेवलपमेंट’), पर्यावरण के साथ मैत्राी वाली प्रौद्योगिकी (‘इको फ्रेंडली टेक्नोलाॅजी’) और प्राकृतिक जीवनशैली (‘नेचुरल लाइफ स्टाइल’) को अपनाना होगा।
संदर्भ
1. ‘पर्यावरण’ वह है, जो हमंे चारों ओर से घेरे है। दूसरे शब्दों में, हमारे ऊपर जो एक आवरण सा है, वही पर्यावरण है। इसके अंतर्गत हमारे आस-पास की वनस्पति, पशु-पक्षी, जल, वायुमंडल, मिट्टी, भू-संरचना इत्यादि शामिल हैं। प्रकृति में सामान्यतः इसके सभी तत्व एक संतुलित अनुपात में रहते हैं। ये तत्व एक-दूसरे पर निर्भर हैं और यदि कोई किसी एक तत्व को भी छेड़ता है, तो प्रकृति-पर्यावरण असंतुलित हो जाता है और इससे मानव-जीवन संकट में पड़ जाता है।
2. सिंह, श्रीभगवान; ‘महात्मा गाँधी के चिंतन में तुलसीदास’, बहुवचन, वर्ष: 3, अंक: 18, जनवरी-मार्च 2002, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), पृ. 113.
ख्नोट: लेखक ने यह बात विशेष रूप से गाँधी के बारे में लिखा है, जो संपूर्ण भारतीय चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं।,
3. शेखर, सुधांशु; गाँधी विमर्श, दर्शना पब्लिकेशन, भागलपुर (बिहार), 2015, पृ. 115-116.
ख्भारतीय मनीषी प्रकृतिपूजक थे और उनके मन में प्रकृति के प्रति विलक्षण प्रेम एवं स्नेह थे। उनका प्रकृति-दर्शन आध्यात्म से ओतप्रोत थे। उनका मानना थे कि समस्त प्रकृति परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर प्रकृति की हर खूबसूरत छटा के बीच छुप कर विहँस रहा है। आसमान में बादलों का प्रवाह, चमकता सूरज, रात्रि में खिला हुआ चाँद, सितारों की टिमटिमाहट, चाँदी सी चमकती मंदाकिनी, ऋतुचक्र की गति, फल एवं फूलों के रंग, फसलों का लहलहाना, उफनती नदियाँ, बहते झरनों का संगीत, लम्बे शाल के वृक्ष, वन्य जीवों का उन्मुक्त विचरण, विविध पक्षियों के मधुर कलरव और भी न जाने कितने रंग हैं, इस मनोहरी प्रकृति के, जिनसे वे अभिभूत थे। वे प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति अतिसंवेदनशील थे और लोगों को बराबर ‘प्रकृति की ओर लौटो’ की शिक्षा देते थे। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति को अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों से श्रेष्ठ माना था। उनकी अहिंसा न केवल जीवित प्राणियों के लिए थी, वरन् निर्जीव भौतिक पदार्थों के लिए भी थी। भूमि का अतिदोहन, उनकी दृष्टि में, उसके प्रति हिंसा करना ही था। उनका दर्शन न केवल मनुष्य एवं जीवित प्राणियों के लिए था, वरन् समस्त सजीव और निर्जीव जगत के लिए भी था।,
नोट: गाँधी के संदर्भ में कही गई यह बात पूरे भारतीय पर लागू होती है।
3. धर्माधिकारी, चन्द्रशेखर; गाँधी-विचार और पर्यावरण, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), प्रथम संस्करण-2009, पृ. 18.
‘अर्थववेद’ में कहा गया है,
ख्”हे धरती माता तुम्हारी टेकड़ियाँ, हिमाच्छादित पर्वत शिखर, तुम्हारे वन, हमारे अंदर की दयाबुद्धि को को जागृत करें भूरी, काली, लाल आदि विभिन्न रंगों की छटाओं से युक्त इस प्रचण्ड धरती का रक्षण इन्द्र करता है। यह अभेद्य, अजेय, अनांकित और अपायहीन है। इस धरती पर मैंने अपना नीड (घर) बसाया है। जिस प्रकार हवा क साथ धूल उड़ती है, ऐसा लगता है कि जगन्नायिका, जगत्तारिणी पृथ्वी ने उस प्रकार मनुष्यों और वृक्षों तथा लताओं को सर्वत्रा फैला दिया है और उनको कलेजे से लगाकर बैठी है।“,
4. गाँधी; हिन्द स्वराज्य, अनुवादक: अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), 2006, पृ. 52.
5. वही, पृ. 52.
6. वही.
7. वही, पृ. 40.
8. गाँधी; हरिजन, वर्ष: 8, अंक: 36.
9. श्रीमन्नारायण; ‘प्राक्कथन’, ग्राम स्वराज्य, लेेखक: गाँधी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद (गुजरात), 2003, पृ. 4-5.
10. गाँधी; हरिजन, 2 नवंबर, 1934, पृ. 301-02.
11. शेखर, सुधांशु; गाँधी विमर्श, पूर्वोक्त, पृ. 118.
12. गाँधी; हिन्द स्वराज्य, पूर्वोक्त, पृ. 94-95.
13. डाॅ. वर्मा, सरोज कुमार; ‘गाँधी-चिंतन में पर्यावरण-चिंता’, दार्शनिक त्रौमासिक, वर्ष: 59, अंक: 3, जुलाई-सितम्बर 2008, प्रधान संपादक: डाॅ. रजनीश कुमार शुक्ल, अखिल भारतीय दर्शन परिषद्, भारत, पृ. 57.
14. गाँधी; हिन्द स्वराज्य, पूर्वोक्त, पृ. 94-95.
15. योजना, वर्ष: 39, अंक: 6, जून 1995, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 13.
16. शेखर, सुधांशु; गाँधी विमर्श, पूर्वोक्त, पृ. 119.
17. कुमार, सुनील; ‘आधुनिक सभ्यता का संकट’, सदभावना साधना, संपादक: स्मिता शाह, मुम्बई (महाराष्ट्र), अगस्त 2009, पृ. 8.