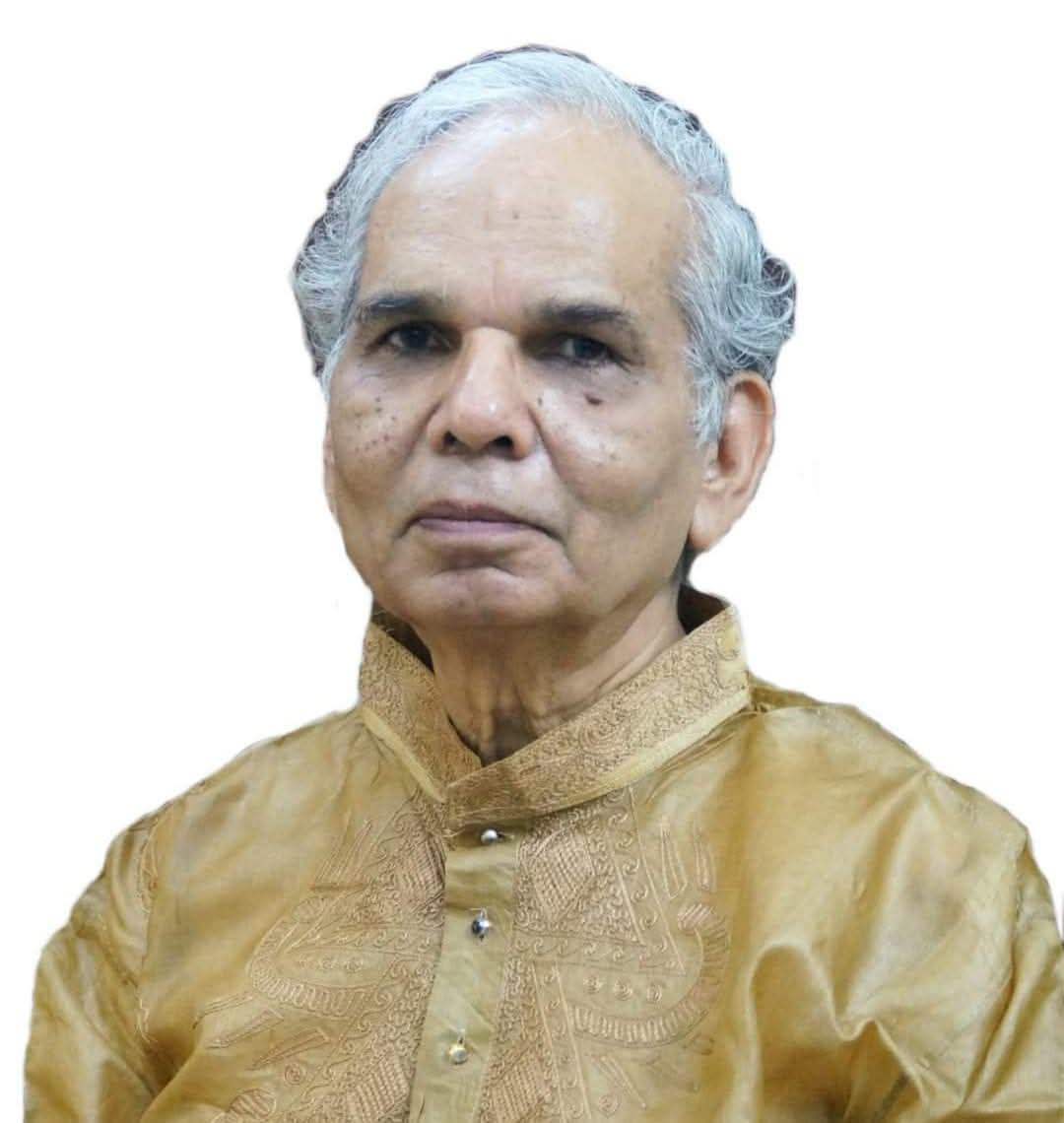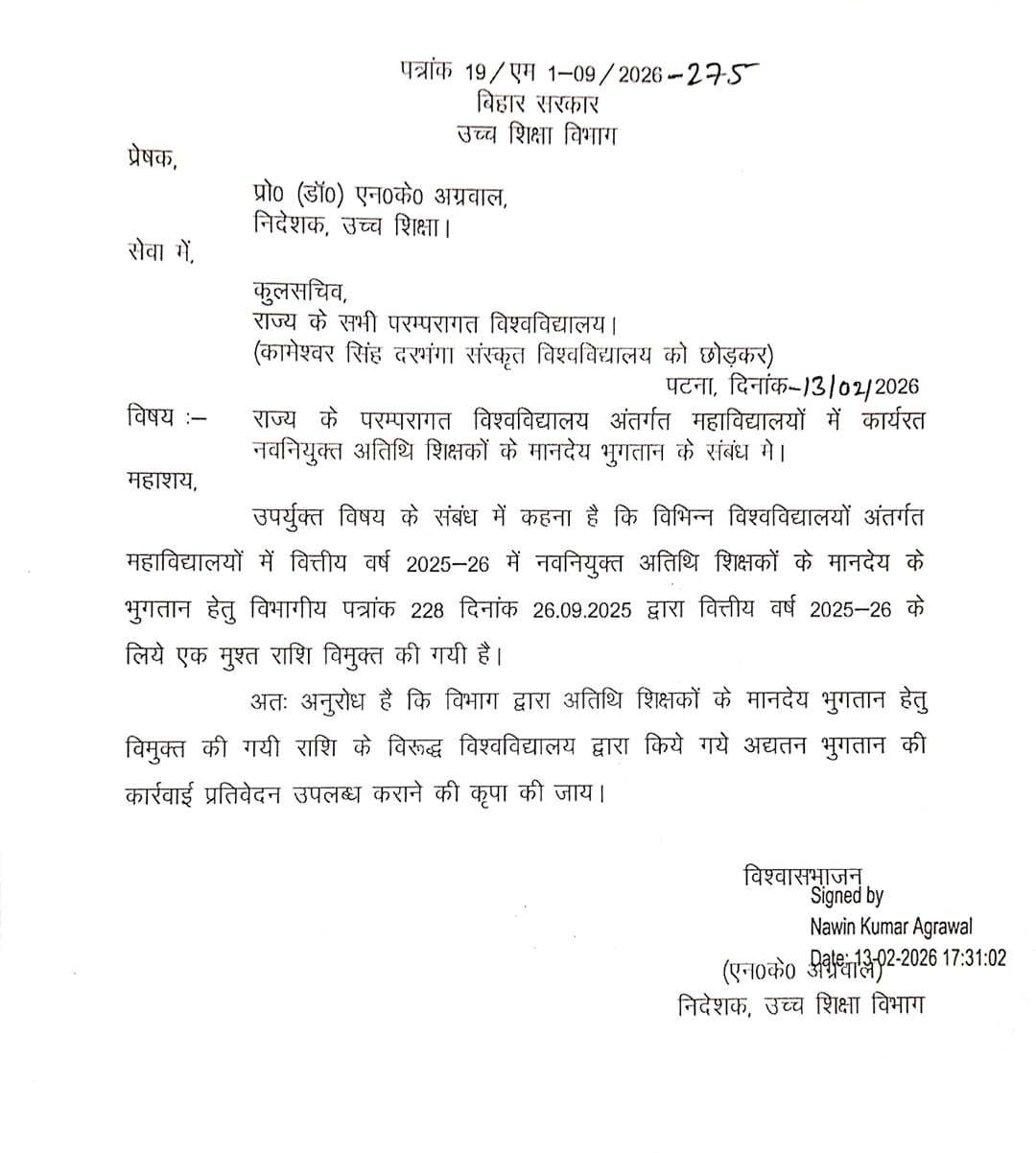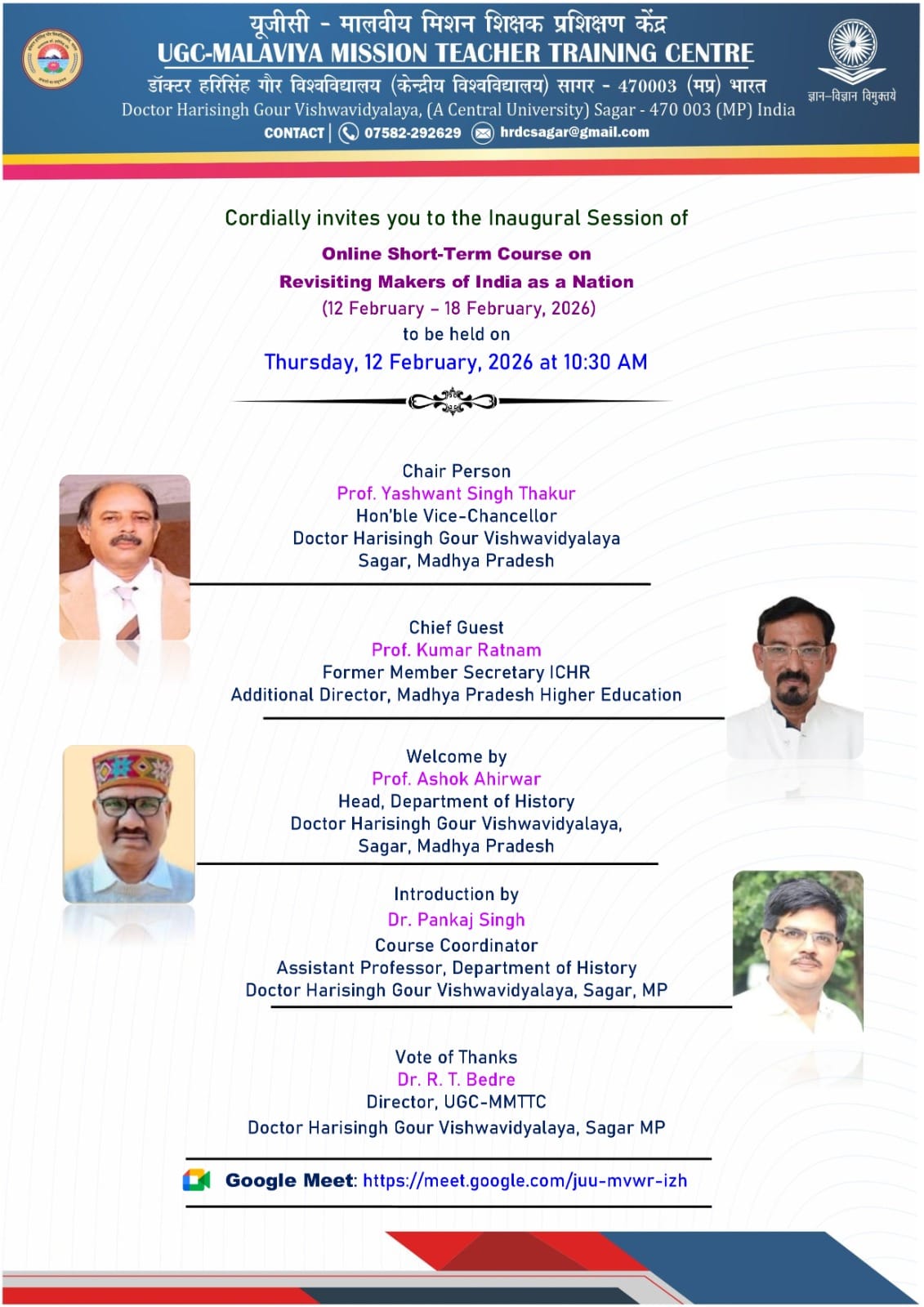4. भूमंडलीकरण और विश्वशांति
भूमंडलीकरण के समर्थक मानते हंै कि दूर-संचार माध्यम और उपग्रह आदि के द्वारा संपूर्ण विश्व सिमटकर एवं वैश्विक परिवार बन गया है, दूरियाँ महत्वहीन हो गई हैं।1 परंतु क्या इस भौतिक सामीप्य ने विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों के दिलों की दूरियों को समाप्त कर दिया है? दूसरा, भूमंडलीकरण के दौरान राष्ट्र-राज्य का क्या होगा? और तीसरा, क्या नैतिक मूल्यों के पुनस्र्थापन के बिना हमारी भौतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति अधूरी नहीं है? अर्थात् क्या बिना नैतिक मूल्यों को आश्रय दिए विश्वशांति एवं विश्वबंधुत्व की स्थापना की जा सकती है? आज इन सवालों का उत्तर देने में भूमंडलीकरण के समर्थक असमर्थ साबित हो रहे हैं।
मालूम हो कि ‘भूमंडलीकरण’ की पहली प्रस्तावना यह है कि विश्व के सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ एकबद्ध या एकीकृत हो गयी हैं। ‘इस मान्यता के पीछे सबसे बड़ा तर्क सीमा-पार व्यापार का है, लेकिन सीमा-पार व्यापार का बढ़ता मूल्य यह प्रस्तावित नहीं करता है कि विश्व के समस्त देशों की व्यवस्थाएँ मिलकर एक हो गई हैं। एकीकरण का एक तात्पर्य समानता भी होगा। अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण लें, तो विश्व में विदेशी निवेश का वितरण सतत् असमान है। … विश्व के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दो तिहाई हिस्सा अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में ही केंद्रित है। इसी तरह विश्व की सर्वोच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 90» मुख्यालय पूर्वोक्त तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। वहीं विकसित देशों में हो रहे कुल घरेलू उत्पादन का 85» हिस्सा उनकी घरेलू जरूरत के लिये ही है।“2
फिर, भूमंडलीकरण का दुहरापन और इसके अंतर्विरोध भी प्रकट हो रहे हैं। एक ओर अमरीका अपने देश के किसानों एवं पशुपालकों को भारी मात्रा में सब्सिडी देता है जबकि वह भारत एवं अन्य देशों की सरकारों को ऐसा करने से रोकता है। अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के बढ़ते वर्चस्व से डरकर अमेरिकी सरकार भारतीयों के काम करने में रोड़ा अटका रही है। सब तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि खुली प्रतिस्पर्धा के नाम पर अमेरिका वैसी बाजी खेलना चाहता है, जिसमें उसकी जीत पूर्वनियोजित हो। एक अजीब विडंबना यह भी है कि उस तथाकथित ‘ग्लोबल विलेज’ में एक जगह (देश) से दूसरे जगह (देश) जाने की खुली छूट नहीं है। दो देशों के बीच लगे कंटीले तारों का घेरा दिन-प्रतिदिन गहरा ही होता जा रहा है और हर देश अपनी-अपनी सैन्य क्षमताएँ बढ़ाने में लगा है। जब पूरी दुनिया एक हो गई है, तो पता नहीं, हम किसके खिलाफ युद्ध की तैयारियाँ कर रहे हैं? लगता है कि हमारे भाग्य विधाताओं को ‘मंगल ग्रह’ जीतने की फिक्र है! डाॅ. अभय ने ठीक ही लिखा है, ”… घृणा, द्वेषमुक्त विकृत मानसिकता एवं स्वार्थवादी क्रियाएँ पूर्ववत् हैं। … आज विश्व के समक्ष मानवता के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। न्यूक्लियर युद्ध में कोई राष्ट्र न विजयी होगा और न दूसरा पराजित। थोड़े से ही परमाणु और हाइड्रोजन बम तथा रासायनिक हथियार इस पृथ्वी को इतना प्रदूषित कर देंगे कि मानव जीवन असंभव-सा हो जाएगा।“3 यहाँ सवाल यह है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका और परमाणु हथियार संपन्न अन्य राष्ट्र ‘व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) को पूरी तरह अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अमेरिका और अन्य परमाणु शक्तियाँ यह चाहती हैं कि उनके पास दुनिया को डराने के लिए परमाणु हथियार तो रहे, लेकिन कोई दूसरा नया राष्ट्र परमाणु हथियार नहीं बना पाए? अन्यथा जिस जैविक एवं रासायनिक हथियारों का झूठा बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक के लोकप्रिय राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को कायरतापूर्ण तरीके से फाँसी पर लटकाया और क्रूरतापूर्वक लाखों इराकी जनता एवं वहाँ की सभ्यता-संस्कृति एवं आस्थाओं को कुचला वैसे हथियार हजारों की संख्या में अमेरिका में क्यूँ रहे? क्या यह दुहरी नीति दुनिया में शांति ला सकेगी? क्या भय द्वारा स्थापित शांति स्थायी हो सकती है? सवाल यह भी है कि अमेरिका-इजराईल जैसे देशों की तानाशाही और उनके द्वारा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन की उन्हें क्या सजा दी जाए? फिर साम्राज्यवादी मूल्कों ने दुनिया के देशों का उपनिवेशकाल में जितना शोषण किया और मूलनिवासियों (रेड इंडियन्स, नीग्रो, आदिवासी आदि) के साथ जो अन्याय किया उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी?
भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व का सवाल भी गौर करने लायक है। आज हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की नीतियों की वजह से विभिन्न देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी है और दुनिया के लोगों में अपने राष्ट्र-राज्य को भूमंडलीकरण रूपी राक्षस से बचाने की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल भूमंडलीकरण एक नव-साम्राज्यवादी साजिश है। इसके जरिए भूमंडलीकरण के पैरोकार विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों को कमजोर कर वहाँ अपना आर्थिक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी देशों की सत्ता बहुराष्ट्रीय निगमों के एजेंटों के हाथों में रहे, किसी राष्ट्रभक्त या जननायक के हाथों नहीं। इसलिए आज का राष्ट्रप्रेम भूमंडलीकरण के प्रतिकूल भले हो, इसे विश्वशांति एवं विश्वबंधुत्व के खिलाफ नहीं माना जा सकता।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक व्यवहार से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक के सीमाविहीन एवं सीमाओं के आर-पार मुक्त संचालन की गतिविधि को वास्तविक मान लेने के परिणाम-स्वरूप ही विभिन्न बौद्धिकों (भूमंडलीकरण के दलालों) को यह साहस हो पाया कि वे कह सकें कि ‘भूमंडलीकरण की प्रक्रिया’ राष्ट्र का अंत है। लेकिन राष्ट्र-राज्य के अंत की घोषणा जितनी दुस्साहसपूर्ण है, उतनी ही छद्म से भरपूर; क्योंकि इसका इस्तेमाल करके साम्राज्यवादी शोषक अपने हितों को पूरा कर पा रहे हैं।’’4 इस बहाने राज्यों के लोककल्याणकारी-लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सामाजिक न्याय की योजनाओं को गैर-उत्पादन मानकर बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। ‘विश्व व्यापार संगठन’ (‘डब्ल्यूटीओ’), ‘वल्र्ड बैंक’ और ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष’ जैसी संस्थाएँ भी दुनिया के विकासशील एवं अविकसित देशों की सम्प्रभु सरकारों को आर्थिक गुलामी एवं कर्ज के जाल में फँसा रही है। जिस ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ को राष्ट्र-राज्य का प्रतिनिधि बताने की कोशिश की जाती है5, उसके ढाँचे में ही लोकतंत्रा बाधित है। लीबिया के तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी के शब्दों में, ”दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद् में विटो प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यों के ‘आतंकवाद’ से त्रास्त है।“6 लेकिन ये तथाकथित आंतकवादी देश लोकतंत्रा एवं शांति के स्वघोषित ठेकेदार बनकर पूरी दुनिया को अशांति फैलाने में लगे हैं और जगह-जगह युद्धरत हैं। हद तो तब हो गई, जब कई देशों में युद्धरत सेना (देश) के कमाण्डर (राष्ट्रपति) को शांति का ‘नोबेल प्राइज’ लेने और अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी एवं साम्राज्यवाद-विरोध के जननायक मार्टिन लूथर किंग को अपना आदर्श बताने में शर्म नहीं आई!
निष्कर्ष: भूमंडलीकरण की पूरी प्रक्रिया मुट्ठी भर पूँजीपतियों के निरंतर विकास और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ‘पूँजी’ ही इसका देवता है और मुनाफा ही ‘मोक्ष’। इसके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है और दुनिया के सारी प्राकृतिक सम्पदाएँ, मनुष्य एवं मनुष्येतर प्राणी महज एक बिकाऊ ‘माल’। इसमें किसी भी चीज का उतना ही मूल्य है, जितना उसका बाजार भाव। भूमंडलीकरण के समर्थक उसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, जिसमें ‘क्रयशक्ति’ होती है या जो बाजार का ‘हितैषी’ होता है। यह उसी राष्ट्र का समर्थन करता है, जहाँ उसका बाजार हित जुड़ा होता है। उसके लिए अपना आर्थिक हित ही सर्वोपरि है और यह आर्थिक हित वैश्वीकरण की दोेहरी नीतियों को बढ़ावा देने से सधता है। जो देश भूमंडलीकरण की नीतियों का विरोध करते हैं, उनका क्या हस्र हो सकता है, यह हम ईराक के मामले में देख चुके हैं। भूमंडलीकरण के समर्थक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सारी सुविधायें, प्राकृतिक संसाधन, मानव श्रम और बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए वह ‘युद्ध एवं प्रेम की नीति’ मानते हैं, जहाँ जीत के लिए ‘सब कुछ जायज है।’ इसी की बानगी है कि राष्ट्र-राज्य के अंत की घोषणा करने वाले देश अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर ‘युद्ध’ को भी ‘जायज’ ठहराते हैं और आर्थिक लाभ के लिए हर जगह अशांति को हवा देने में लगे रहते हैं। अतः, अब समय आ गया है कि हम ‘विश्वशांति’ को सही संदर्भों में देखें-समझें।
संदर्भ
1. सिंह, डाॅ. अभय कुमार; ‘वैश्वीकरण एवं विश्वशांति’, दार्शनिक अनुगूंज, वर्ष: 2, अंक: 1, जनवरी-जून 2010, का. संपादक: डाॅ. श्यामल किशोर, दर्शन परिषद्, बिहार, पटना (बिहार), पृ. 63.
2. सिंह, कंवलजीत; वैश्वीकरण?, अनुवाद: जीतेंद्र गुप्त, संवाद प्रकाशन, मुंबई (महाराष्ट्र), 2008, पृ. 9.
3. सिंह, डाॅ. अभय कुमार; ‘वैश्वीकरण एवं विश्वशांति’, दार्शनिक अनुगूंज, वर्ष: 2, अंक: 1, 20, पूर्वोक्त, पृ. 64.
4. सिंह, कंवलजीत; वैश्वीकरण?, पूर्वोक्त, पृ. 9.
5. सिंह, डाॅ. अभय कुमार; ‘वैश्वीकरण एवं विश्वशांति’, दार्शनिक अनुगूंज, वर्ष: 2, अंक: 1, जनवरी-जून 2010, पूर्वोक्त, पृ. 64.
6. वही.