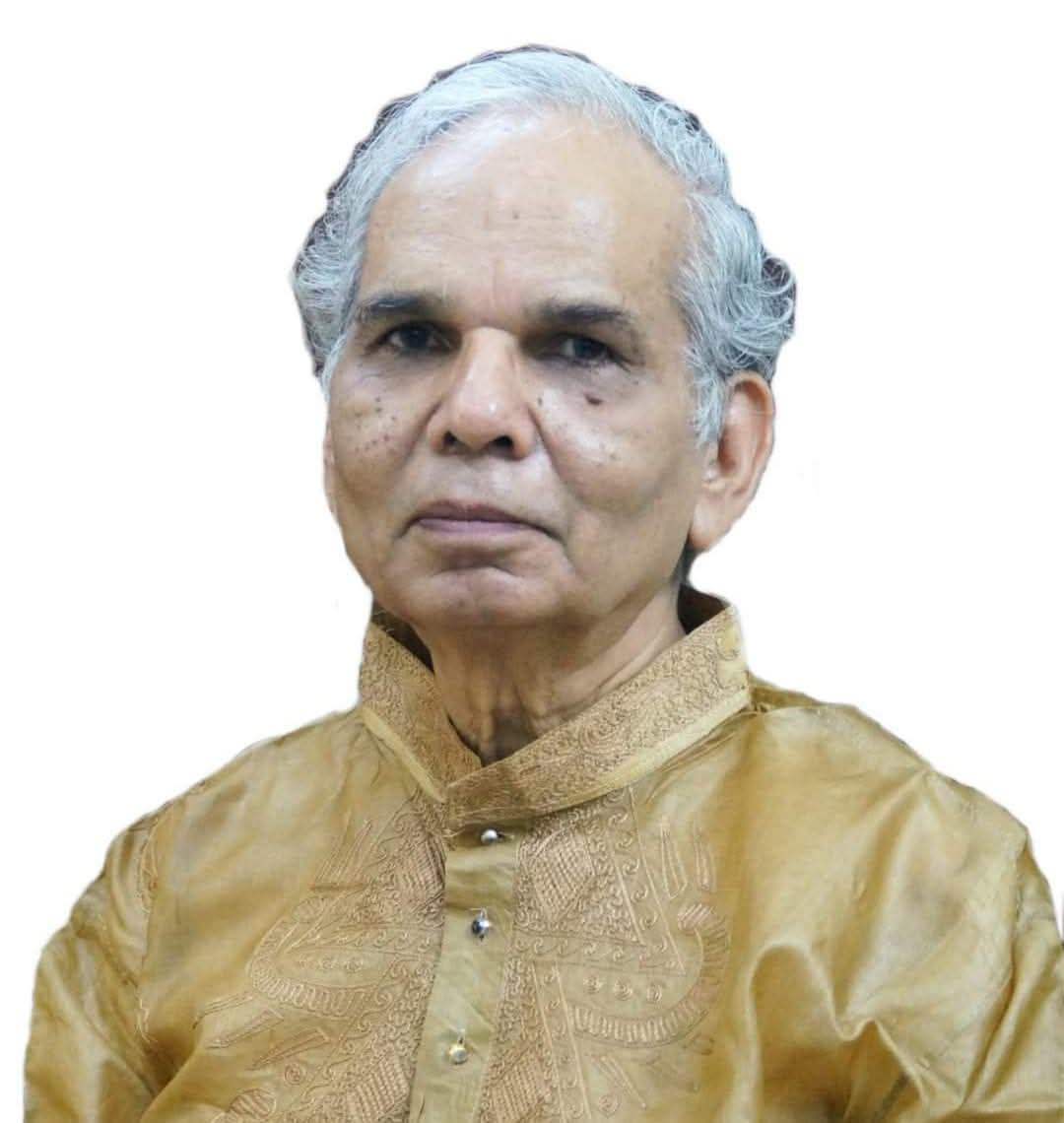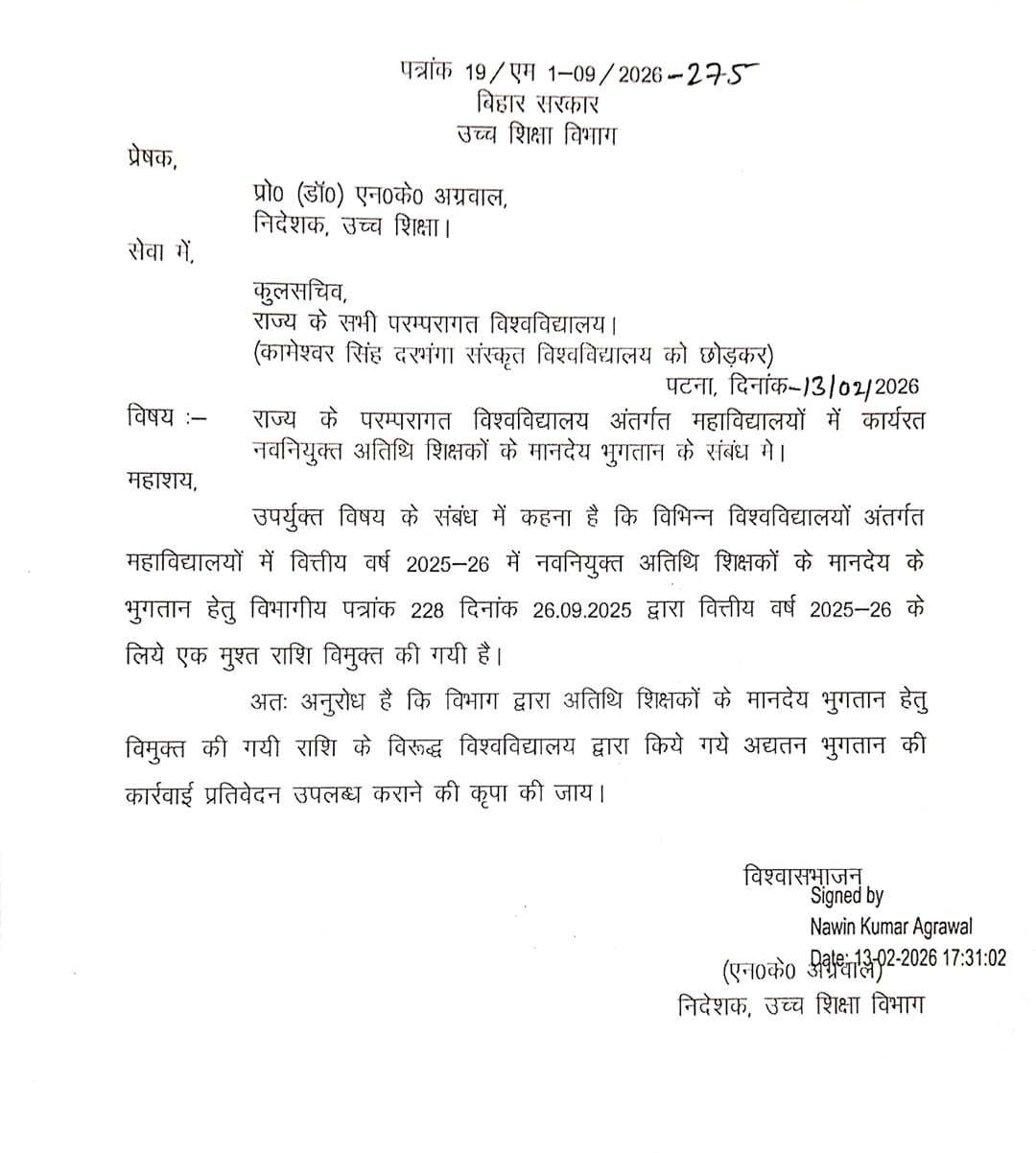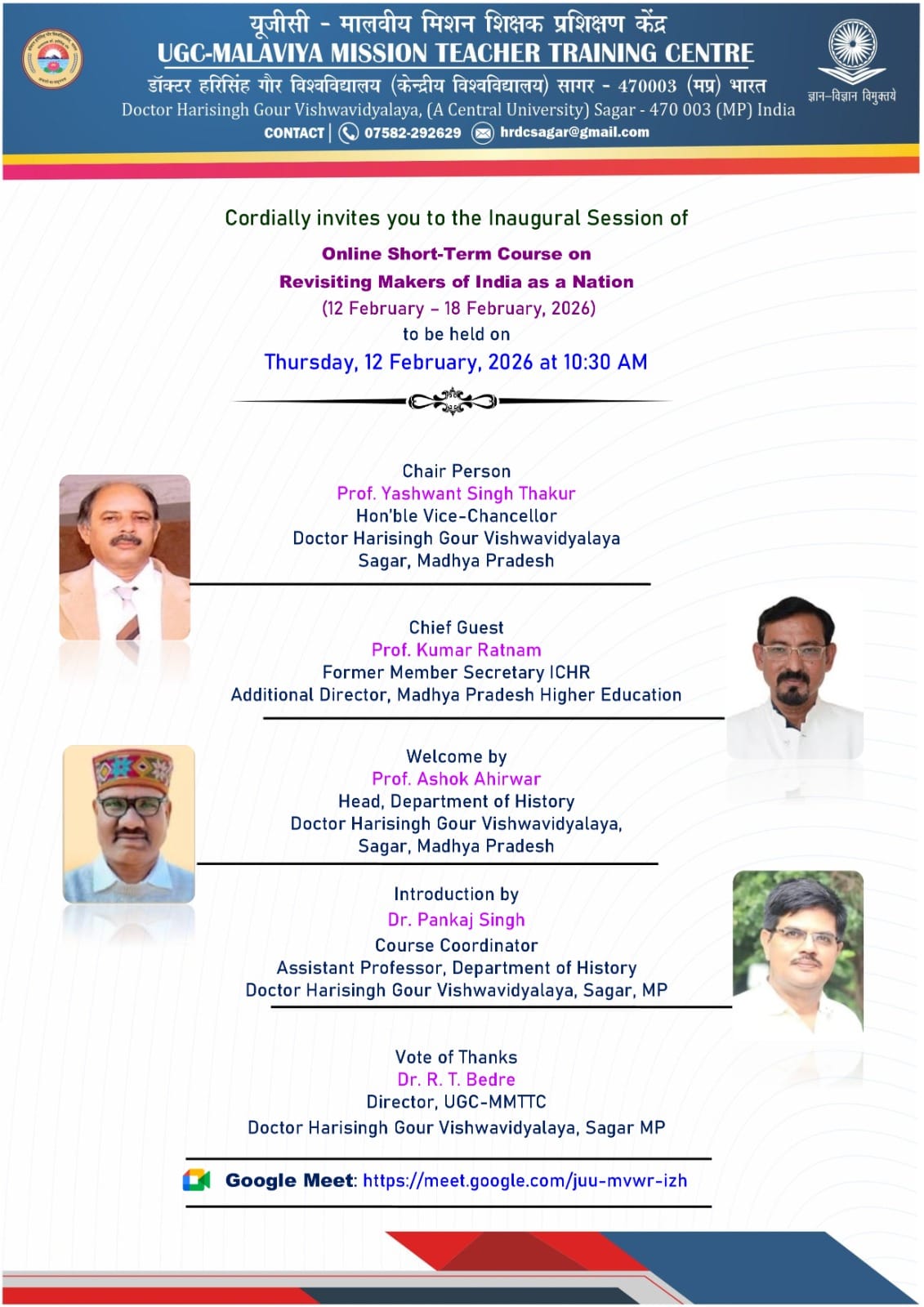शीर्षक : क्या यही है धर्म सिखाता तुमको?
शर्मिंदा कर गई आज फिर एक बेटी,
बड़ा गर्व करते हो अपने धर्मों पर,
पल पल लड़ते मरते हो अपने धर्मों पर,
पर क्या यही धर्म सिखाता तुमको?
निर्बल असहायों को दबोचना,
नोंचना,
रोंदना,
वीभत्सता की हदें पार करना,
भूखे गिद्दों की तरह टूटना,
इतना ही काफी नहीं,
धर दबोचना,
उतने पर भी संतुष्टि नहीं,
बोटी बोटी नोंचना,
फिर हाड़मास दोनों को,
ज़िंदा फूंकना,
न विस्मृत हो उसे की वो नारी है,
मत भूल पुरुष से तू सदियों से हारी है।
रह औकात में,
मत भूल तुझ पर अधिकार अपना,
हमारी भूख मिटाना बस है,
काम तेरा,
इसके ऊपर न कोई अस्तित्व तेरा,
झुका कर आँख चल,
नज़रें उठाने की जुर्रत न करना,
नहीं तो जान ले कि,
क्या होगा फिर हस्र तेरा।
घड़ी घड़ी है जो याद दिलाता,
तू हदें हमको,
क्या बस यही सिखाता है,
ये धर्म तुझको?
क्या कभी उसने तुझको ये बताया नहीं,
बिना मेरे तू इस जहान में आया नहीं,
घमंड किस बात का करता,
तू अपनी नस्ल पे है,
मेरे बिना जो संभव ही नहीं????
मेरे धर्म ने तो बस मुझको खाया इतना,
भूलकर खुद को खुशियां देना सबको,
इंसानियत ही धर्म और कर्म है मेरा,
जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं तेरा।
तेरे धर्म की किताब,
तूने ही लिखी होगी,
वरना कोई धर्म आपस में लड़ाता है नहीं,
स्त्री-पुरुष, जात-पात, ऊंच-नीच का भेद बताता है नहीं,
समानता ही उसकी सरस परिभाषा है,
जानवर वो किसी को कभी बनाता है नहीं।
सच तो ये है कि हैवानों की कोई जात,
कोई धर्म है ही नहीं,
वो तो बस धर्म को बदनाम करने का,
एक ज़रिया हैं,
वो तो केवल एक अपवाद हैं,
इसके सिवा और कुछ भी नहीं।
डॉ० दीपा
सहायक प्राध्यापिका
दिल्ली विशवविद्यालय