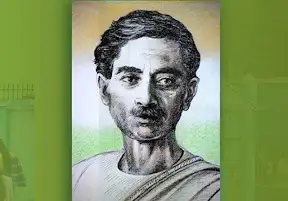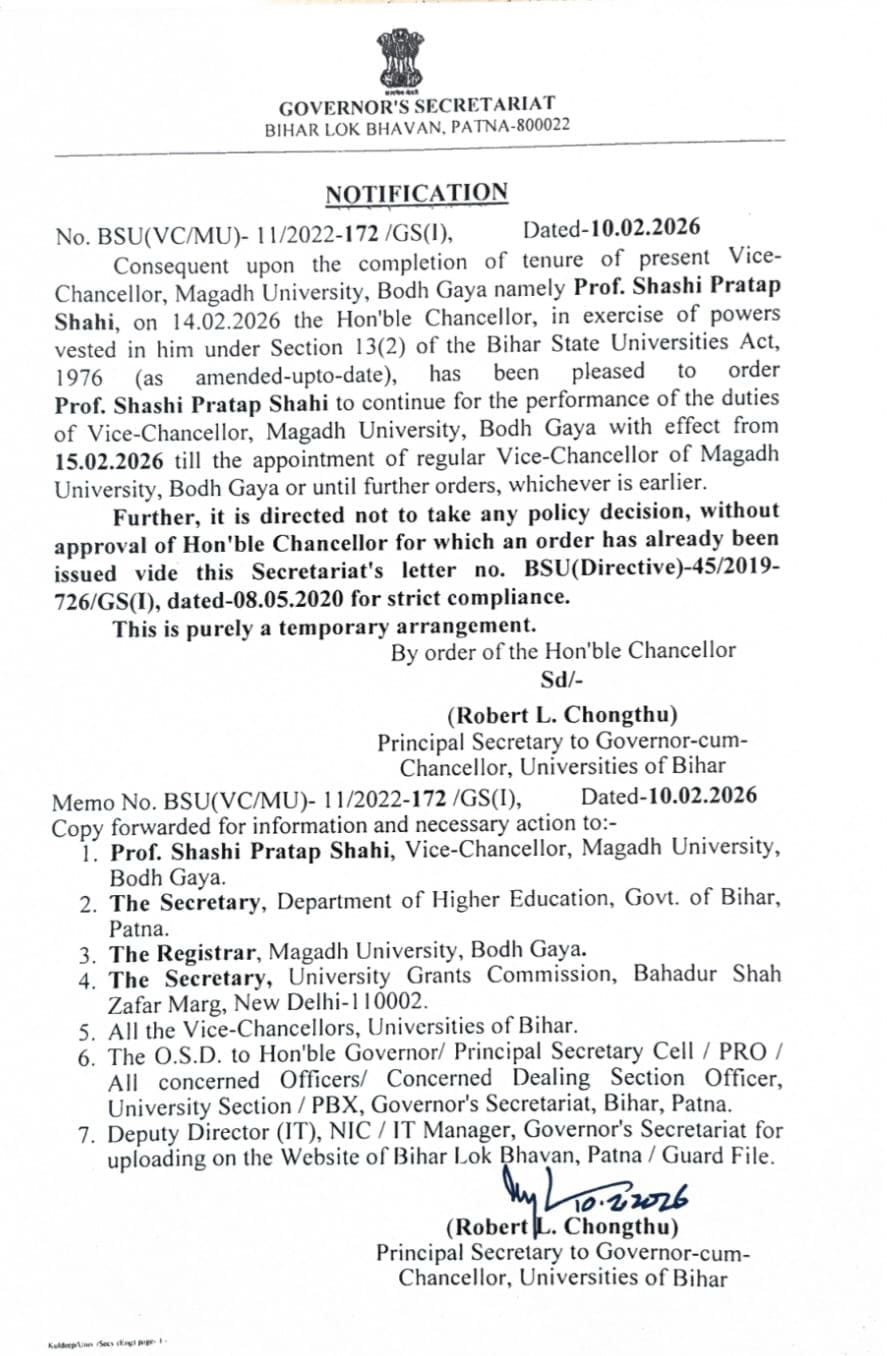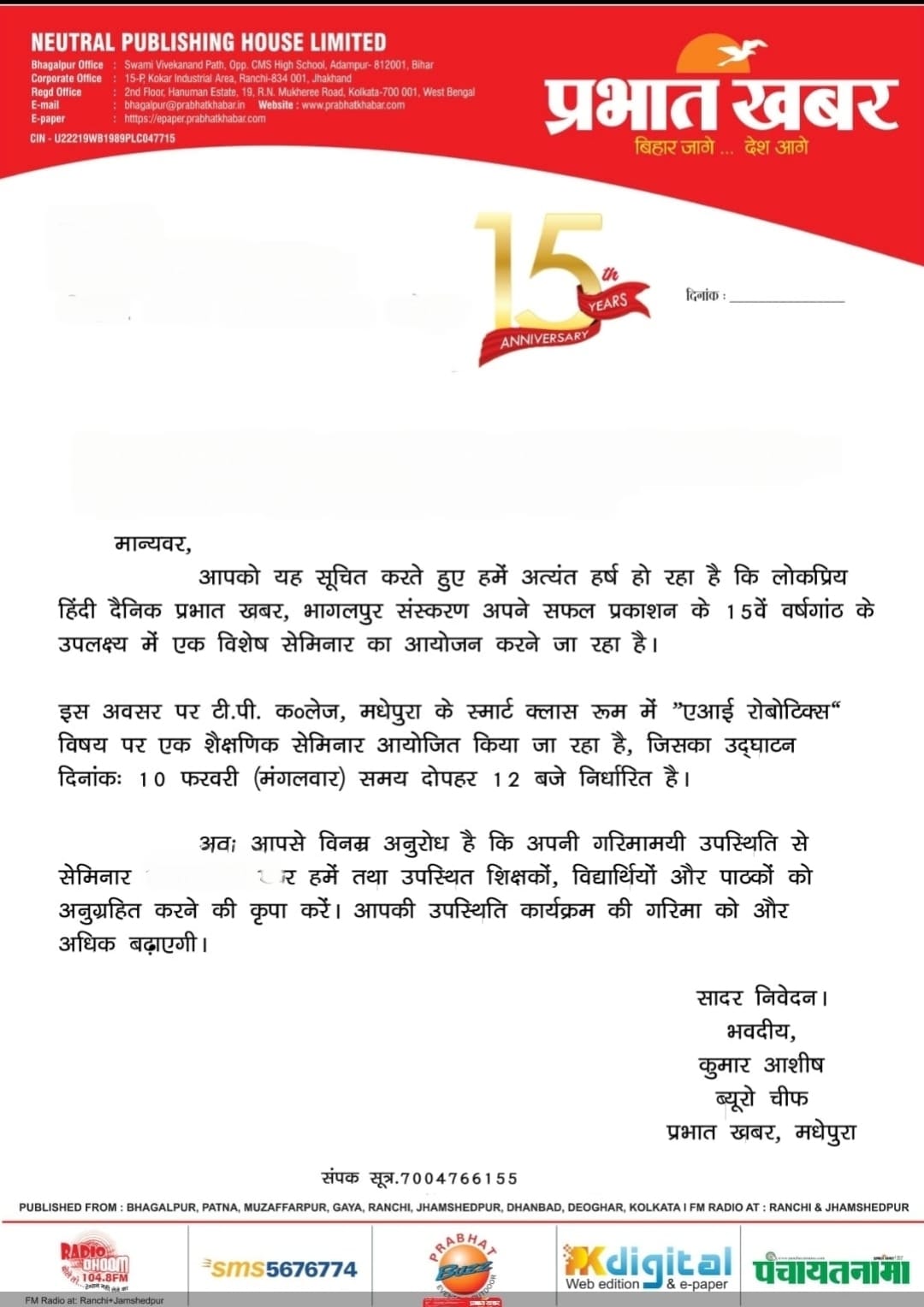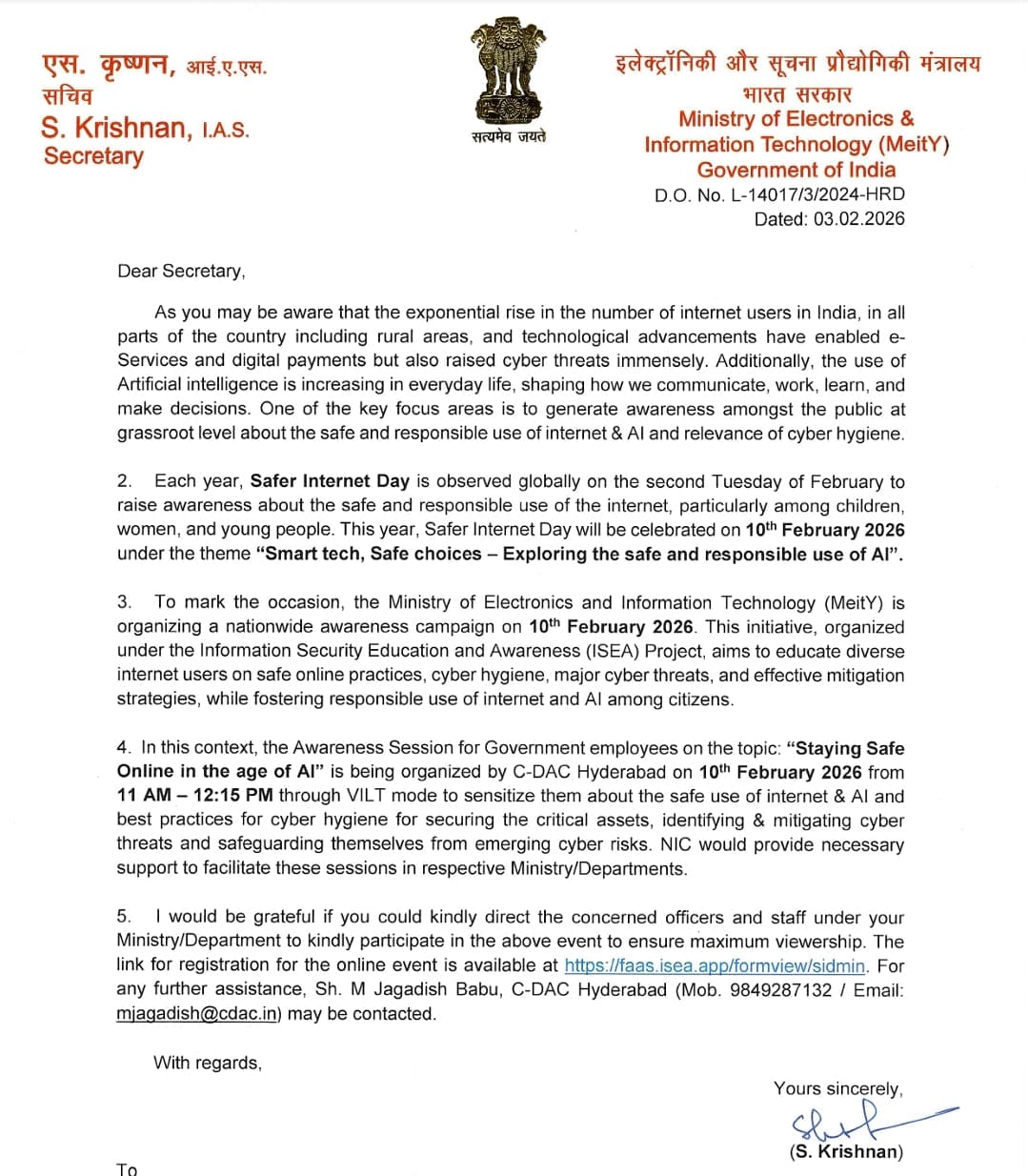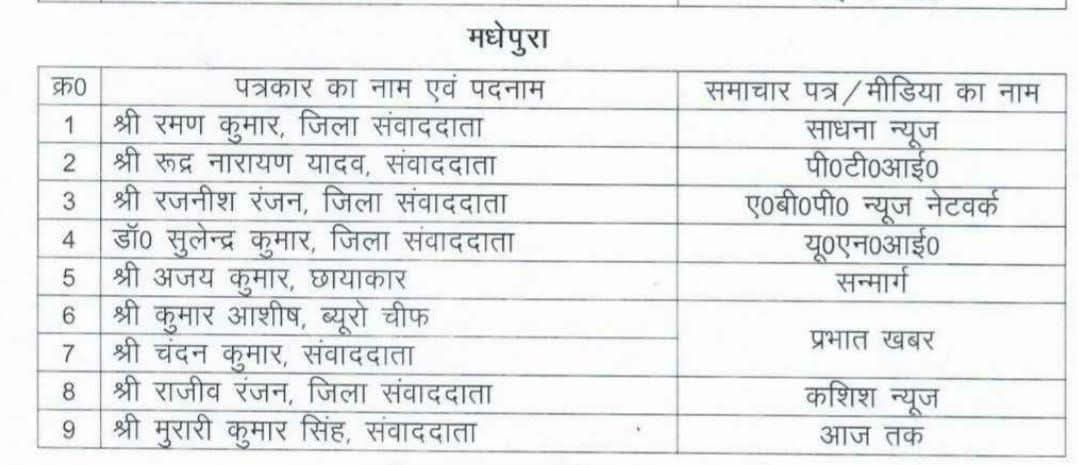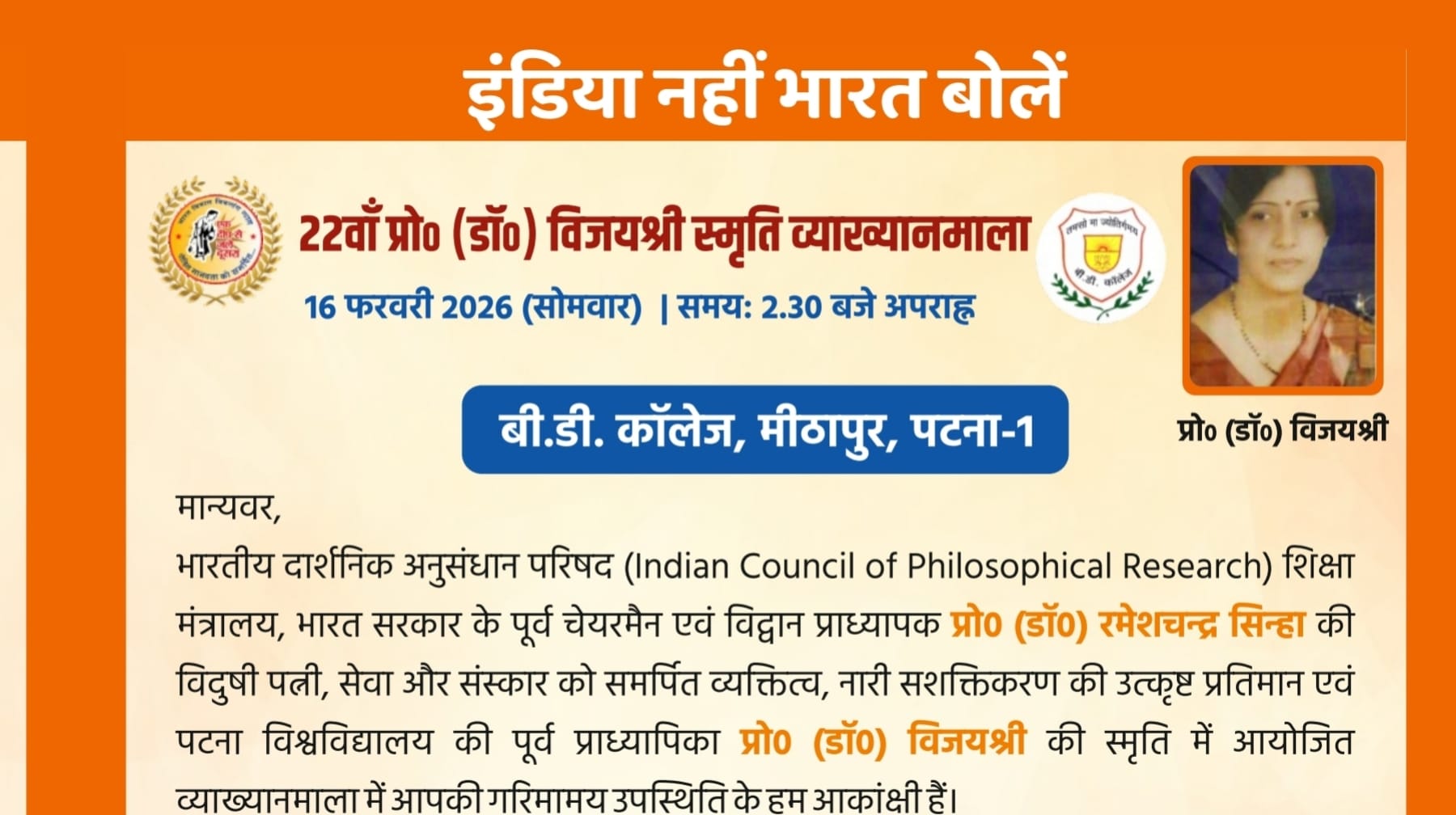प्रेमचन्द की हिन्दी का हाल
प्रेमकुमार मणि
भारतेन्दु के ज़माने से जोड़ लिया जाय तो आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास लगभग डेढ़ सौ साल का है. इसी काल में ब्रजबोली और अन्य बोलियों से निखर कर खड़ी बोली एक भाषा के रूप में विकसित हुई और भाषा के नये ठाट में इसके पद्य और गद्य लेखन का आरम्भ हुआ. आलोचक शिवदान सिंह चौहान बस इसी दौर को हिन्दी साहित्य कहते थे. इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना सच तो है ही कि भारतेन्दु पूर्व का जो साहित्य हिन्दी के नाम पर चल रहा है वह आधुनिक हिन्दी साहित्य नहीं है. उसकी पृष्ठभूमि भले हो.

इस आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी विकास के कई पड़ाव हैं. उन्नीसवीं सदी के आखिर में हमारे देश-समाज में आधुनिकता के साथ जिन मनोभावों का विकास हुआ साहित्य उसकी परछाई के रूप में आया. प्रेमचंद की कामना थी कि साहित्य समाज का दर्पण या छाया न हो कर उसे रास्ता दिखाने वाला टॉर्च-लाइट अथवा मशाल बने. यह भाव उन्होने 1936 के एक भाषण में व्यक्त किया था. दर्पण और मशाल का कश्मकश हमारे साहित्य में हाल तक दीखता रहा. प्रेमचंद के जमाने तक अधिकांश लोग साहित्य को मनबहलाव का साधन माने बैठे थे. वे उसमें रस की तलाश करते थे. हमारे भारतीय काव्य शास्त्र,जो कि संस्कृत काव्य-शास्त्र था, की अपनी मान्यताएं थीं. उसके रस-सौंदर्य की अपनी कसौटी थी. लेकिन प्रेमचंद जैसे लेखक देख रहे थे कि समाज में जद्दो-जहद छिड़ चुका है और आज इस समाज को रस की जगह नये विचार की जरूरत है. आधी सदी पहले 1857 में रजवाड़ी ताकतों और पुराने सामाजिक सोच वाले लोगों ने मिल-जुल कर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक विद्रोह किया था. इनकी कोशिश एक बार फिर पुराने ज़माने में जाने की थी, जहाँ वे अपेक्षाकृत सुकून महसूस कर रहे थे. जैसा कि 1850 के दशक में कार्ल मार्क्स ने अपने भारत विषयक लेखों में बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में सामाजिक रस्साकशी चल रही है. ब्रिटिश शासन ने परंपरागत सुस्त उत्पादन प्रणाली में थोड़ा-सा ही सही हस्तक्षेप किया है और यही इस चिल्ल-पों का कारण है. मार्क्स ने कुल मिला कर भारतीय सामाजिक अंतर्विरोधों पर एक विहंगम नजर ही डाली थी, किन्तु वह समझ सका था कि एक सुस्त और पुरानी पड़ चुकी उत्पादन प्रणाली ने जटिल और ठहरे हुए जातिवादी समाज को रचा है. इसलिए भारत में अंग्रेजी राज को वह इतिहास का अवचेतन साधन मान रहे थे, जो जाने-अनजाने परम्परागत उत्पादन प्रणाली को तोड़ रहे थे. जर्मन कवि गेटे की एक पंक्ति उद्धृत करते हुए उन्होंने बतलाया कि वह दुःख महान है, जो एक महान सुख को जन्म देता है. मार्क्स की नजर में अंग्रेजों के आने का दुःख ऐसा ही था.
1857 में पुराने ख्याल के लोग पिट गए. कोई नहीं जानता कि वे यदि सफल हो जाते तो क्या होता. सावरकर ने उसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना और आगे चल कर रामविलास शर्मा ने उसे हिन्दी नवजागरण से जोड़ा. उसकी तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की. लेकिन यह एक अजीब संयोग है कि उस दौर में सामाजिक नवजागरण से जुड़े लोगों ने या तो इस बगावत का विरोध किया या फिर इस से तटस्थ रहे. जोतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान और बंगला रेनेसां से जुड़े लगभग सभी लोगों ने इससे स्वयं को अलग रखा. इन अन्तरविरोधों की अभी कोई गहरी मीमांसा नहीं हुई है.
1857 की घटना ने बहुत कुछ बदल दिया था. ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश रूल भारत में आ गया और अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के बारे में नए ढंग से सोचना शुरू किया. ब्रिटेन में भी विभाजित समाज था. वहां भी लार्ड और कॉमन लोग थे. उनकी सोच अलग-अलग थी. लेकिन वह समाज रेनेसां और प्रबोधन से गुजर चुका था और वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी. क्राउन अवश्य था, लेकिन वहां संसदीय राजनीति चल रही थी. यही कारण था कि किसी न किसी अंश में उनका प्रभाव भारत पर पड़ा. एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने कोलकाता युनिवर्सिटी के स्नातकों के नाम एक पत्र लिख कर उन्हें अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों का ख्याल कराया और अंततः दिसम्बर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो आगे चल कर इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन का वाहक बना.
हिन्दी साहित्य इसी के समान्तर विकसित हुआ. भारत की अन्य आधुनिक भाषाओँ का विकास भी लगभग इसी दौर में हुआ. यह शायद इसलिए कि पढ़े-लिखे लोगों के बीच संवाद की जरूरत बढ़ती गई. प्रेस और पत्र-पत्रिकाओं का विकास भी हुआ. 1920 तक देश के विभिन्न हिस्सों में न केवल राष्ट्रवादी नेता नजर आने लगे बल्कि विभिन्न देशी जुबानों में आधुनिक गद्यकार भी दिखने लगे. कहानी, उपन्यास और विभिन्न विषयों पर निबंध-लेखन भी इसी दौर में तेजी से हुआ.
हिन्दी में प्रेमचंद सर्वमान्य रूप से एक मुकम्मल लेखक के रूप में उभर कर आए. हमारे पड़ोस में रवीन्द्रनाथ टैगोर और शरतचंद्र बंगला में आए. गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलगु सभी जुबानों में नए मिजाज के लेखकों का प्रादुर्भाव हुआ. यह सब एक नयी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता थी, जिस का तुलनात्मक अध्ययन अभी कम ही हुआ है.
यूरोपीय समाज में विभिन्न जुबानों का आधुनिक साहित्य रेनेसां, प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति और संसदीय राजनीतिक सोच से प्रभावित रहा. भारत में रेनेसां की परछाई पड़ी थी. बंगाल, महाराष्ट्र और द्रविड़ क्षेत्र का नगर समाज इस से प्रभावित हुआ. राजा राममोहन राय (1772-1833), जोतिबा फुले(1827-1890), इयोती थास(1845-1914) और नारायण गुरु (1856-1928) जैसे सामाजिक दार्शनिकों ने एक नये सोच को जन्म दिया था. हिंदी समाज में ऐसा कुछ नहीं हुआ. यहाँ सामाजिक परिवर्तन की सोच कुछ देर से अंकुरित हुई और उसका केंद्र लाहौर रहा. बनारस एक बुझी हुई सोच का नगर था, जहाँ मध्यकाल में कबीर ने तो ताल जरूर ठोकी थी आधुनिक ज़माने में पण्डे -पुरोहितों की चलती थी. प्रेमचंद इसी नगर से जुड़े थे. यहाँ उन्हें नवजागरण का शंखनाद करना था. उनका काम जरा मुश्किल था.
प्रेमचंद आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढे. उन्होंने साहित्य को किसानों के नजरिये से देखा, गाँव के नजरिये से नहीं. उनका प्रथम कहानी संग्रह ‘ संसार का सब से अनमोल रतन ‘ 1909 में प्रकाशित होता है. ठीक इसी वर्ष रवि बाबू के महत्त्वपूर्ण उपन्यास गोरा का प्रकाशन होता है और महात्मा गांधी की वैचारिक पुस्तिका ‘ हिन्दस्वराज ‘ भी इसी वर्ष प्रकाशित है.
प्रेमचंद बनारस और उसके पास के गाँव लमही से जुड़े हैं. पेशा से स्कूल मास्टर हैं. उनके बनारस में बुद्धिजीवियों की कोई ऐसी जमात नहीं है, जहाँ बैठ कर वह कोई विमर्श करते हों. हिन्दी भाषी समाज में सामाजिक विमर्श के नाम पर वर्णधर्म की चिन्ता की जाती है. इसी के बीच से एक देश-समाज या राष्ट्र विकसित करने कोशिशें जारी हैं. कल्पना कर सकते हैं कि प्रेमचंद की मानसिक स्थिति कैसी होगी. 1924 में उनकी एक कहानी प्रकाशित होती है ‘ शतरंज के खिलाड़ी ‘. यूँ है तो यह एक कहानी, लेकिन आप इसे जब पढ़ते हैं तब एक निबंध का बोध होता है. वह पाठकों से सीधा संवाद कर रहे हैं. अवध का पतन कैसे और क्यों हुआ? उसका केंद्र लखनऊ किस तरह विलासिता में डूबा था. उत्पादन भी हो रहा है तो विलासिता के सरंजाम भर के. कपड़ों पर कसीदे सजाए जा रहे हैं, सुरमे और कुमकुम बन रहे हैं. अहदीपन की हद है. सामंतवाद चरम पर है. सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का नाम नहीं. ऐसे समाज को गुलाम होने से कौन रोक सकता है. अंग्रेजी फौजी कुमुक एक रोज आती है और बिना कतरा भर खून बहाए अवध के नवाब को उठा ले जाती है. यह भारत का पतन नहीं,सामंतवाद का पतन था. यही लोग अंग्रेजी राज से लड़ने का दम्भ भर रहे थे.
प्रेमचंद उन इतिहासकारों के सामने सवाल खड़े करते हैं जो लगातार फलसफे पेश किये जा रहे थे कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों की मक्कारी और फरेब से पराजित हुए. प्रेमचंद आँखों में आँख डाल कर हकीकत बयां करते हैं. नहीं, उनके फरेब से नहीं आप अपनी विलासिता और अहदीपन के कारण हारे. अपने पूरे साहित्य लेखन में प्रेमचंद ने यही बताया कि हम ने अपने ही भारतीय समाज को विभाजित रखा. जातपात के खांचे बना कर रखे और ऐसी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था बनाई कि मिहनत करने वाले लोग सताए जाएँ और उनकी कमाई पर बैठे-ठाले सामंत और पुरोहित तबके के लोग गुलछर्रे उड़ाएं.
प्रेमचंद का साहित्य ब्रिटिश राज के प्रति उतना मुखर नहीं है जितना कि अपने हिंदुस्तानी जमींदार-पुरोहित वर्ग के प्रति. सामंत और पुजारी तबका जब समाप्त होंगे ब्रिटिश इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे. देश के असली दुश्मन ये भीतरी लोग हैं. कुछ ऐसी ही बातें वाल्तेयर अपने मुल्क में करते थे. बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध को देखें तो हिन्दी भाषी समाज में जो चुने हुए सामाजिक विमर्शकार हैं उनमें प्रेमचंद हैं. अन्य उल्लेखनीय लोगों में जवाहरलाल नेहरू, राहुल सांकृत्यायन और भगत सिंह हैं. लेखकों की जमात जरूर विकसित हुई है, लेकिन ज्यादातर कलमघिस्सू हैं या फिर वर्णधर्म केंद्रित राष्ट्रवाद के उन्नायक जोशीले वन्दे मातरमी लोग.
क्या सचमुच प्रेमचंद की कोई परंपरा हिन्दी में विकसित हुई. मेरा जवाब होगा हुई, लेकिन दबा दी गई. प्रेमचंद की एक परंपरा यशपाल, रांगेय राघव जैसे लेखकों में तो दूसरी जैनेन्द्र, अज्ञेय और रेणु जैसे लेखकों में विकसित हुई. कोई भी जान सकता है कि उनकी परम्परा के असली कातिल कौन लोग थे. इस परम्परा के कमजोर होते ही हिन्दी साहित्य का बैताल एक बार फिर अपने पुराने डाल पर जा बैठा.
यह सब कैसे हुआ? प्रेमचंद की परंपरा के असली कातिल वे लोग थे, जो उनकी माला सब से अधिक जप रहे थे. प्रेमचंद के ज़माने में वन्दे मातरमी मिजाज के राष्ट्रवादी भारत वंदना और उपनिवेशवाद विरोध केलिए सामाजिक प्रश्नों को अनसुना करते थे. आज़ादी के बाद उपनिवेशवाद विरोध की जगह पूंजीवाद विरोध को लक्ष्य मान लिया गया और इसकी केन्द्रीयता भंग न हो इसके लिए सामाजिक प्रश्नों पर चुप्पी साध ली गई. हिंदी साहित्य पूंजीवाद विरोध का साहित्य बनता चला गया, जो यहाँ ठीक से विकसित भी नहीं था. सामंतवाद और पुरोहितवाद के खिलाफ संघर्ष शिथिल कर दिया गया. यह एक ट्रेजेडी बन गई. हुआ यह की प्रेमचंद की परंपरा के नाम पर एक कृत्रिम सोच का साहित्य लिखा जाता रहा. कृत्रिम विचार और कृत्रिम यथार्थ ने मिल कर साहित्य की एक विकलांग परंपरा विकसित की.
प्रेमचंद की परंपरा अंततः मर गई. आज का पूरा हिन्दी साहित्य एक बार फिर विलासिता और भाषा का खिलवाड़ बन कर रह गया है. यह विचारशून्य साहित्य है. विश्वविद्यालयों में तंग-दिमाग प्रोफेसरों की भरमार है, ज़िन्होने साहित्य को एक घेरे में बाँध रखा है. इन लोगों ने स्वयं को साहित्य का पुरोहित मान लिया है. पतरा बांचने की तरह ये आलोचना लिखते हैँ और लगातार धुंध फैलाते हैँ. हर वर्ष हजारों ज़िल्दें छपती हैँ, पुरस्कृत होती हैं और फेंक दी जाती हैं. कहीं कोई सामाजिक विमर्श नहीं होता. यही वह दौर रहा जब हिन्दी पट्टी में दक्षिणपन्थी वैचारिकता का तेजी से विकास हुआ. मार्क्सवाद का लबादा ओढ़े बैठे लोग अचानक से या तो तटस्थ हो गये या फिर हवा में बह गए. वे कल भी सुखी थे आज भी सुखी हैँ. साहित्य कुल मिलाकर प्रोफेसरों, अधिकारियों और दूसरे वर्चस्व प्राप्त लोगों का शगल बन कर रह गया है. अपने चरित्र में पूर्व की अपेक्षा आज यह अधिक द्विजवादी है. न यहाँ कोई सामाजिक विमर्श है, न अपने समय के मिथ्याचार को समझने की परिदृष्टि. इक्कीसवीं सदी का साहित्य ऐसा हो नहीं सकता. अपने समय के जटिल यथार्थ और प्रश्नों से उसे टकराना ही होगा. विचार आज के साहित्य का मुख्य केन्द्रक है, या होना चाहिए. यह नारेबाजी का दौर नहीं है. लोगों ने देखा जॉर्ज लूकाच (1885-1971) जैसे दिग्गज आलोचक को आज की दुनिया ने इस आधार पर नकार दिया कि वे अपने समय के अंतर्विरोधों का आकलन नहीं कर सके. मैक्सिम गोर्की का आकर्षण उनके ही रूस में कमजोर पड़ गया, लेकिन टॉलस्टॉय और चेखब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे तो अपने साहित्य के सरोकारों का ज्ञान भी हो जाएगा.
प्रेमचन्द अजूबे लेखक थे. उन्हें समझने केलिए हमें किताबों से अधिक विवेक की जरूरत होगी. लोगों ने उनकी परंपरा के नाम पर कबाड़ इकठ्ठा किया है. इससे बचना होगा. प्रेमचंद की परंपरा का अर्थ है वैज्ञानिक नजरिये से अपने समय के प्रश्नों से टकराना और उनके जवाब ढूंढना. आज वह होते तो इस समय के सवालों के सार्थक जवाब तलाशने की कोशिश करते. कम से कम उन तमाम मिथ्याचारों की कलई तो खोलते ही जो यथार्थ के नाम पर हो रहा है.