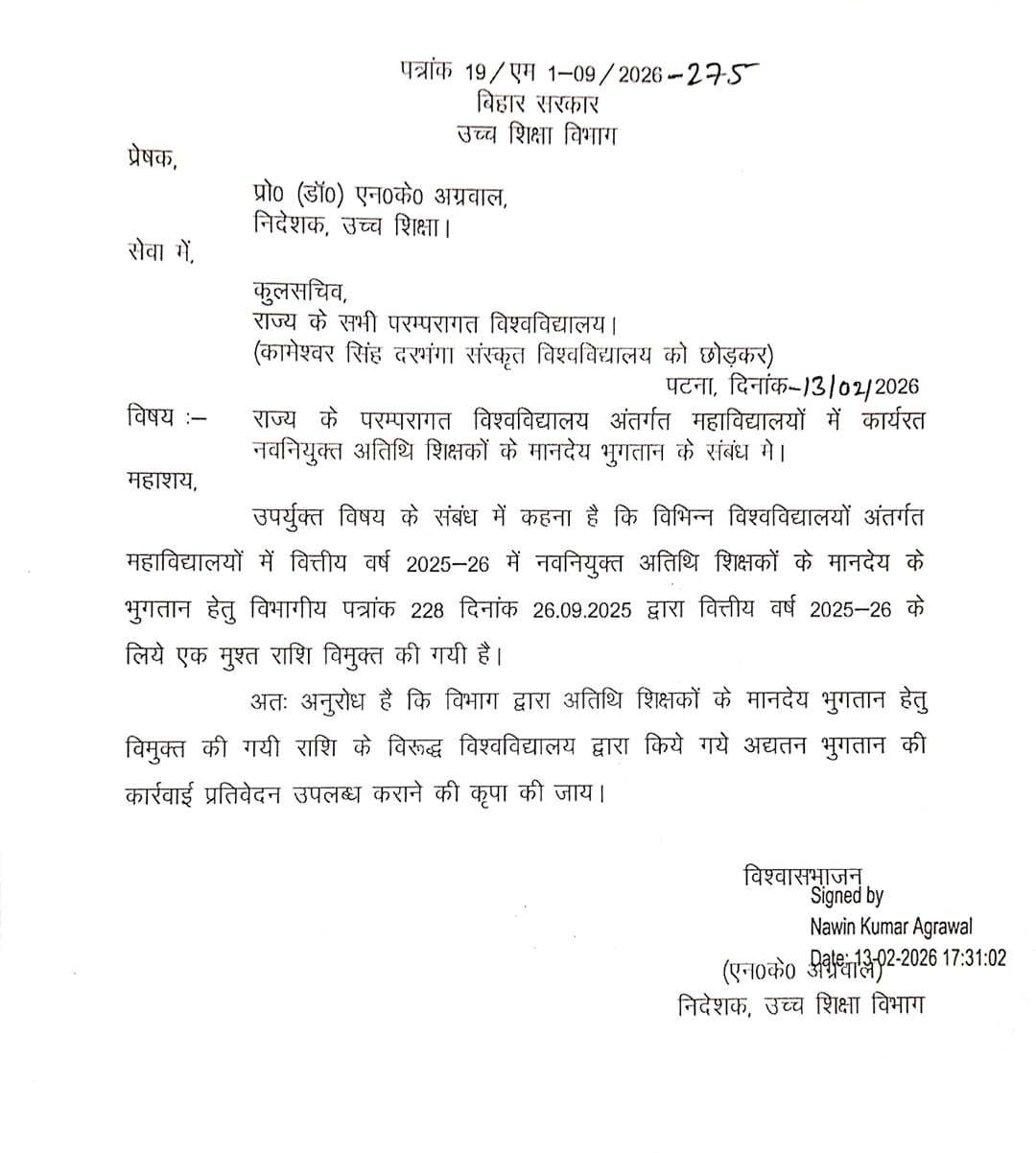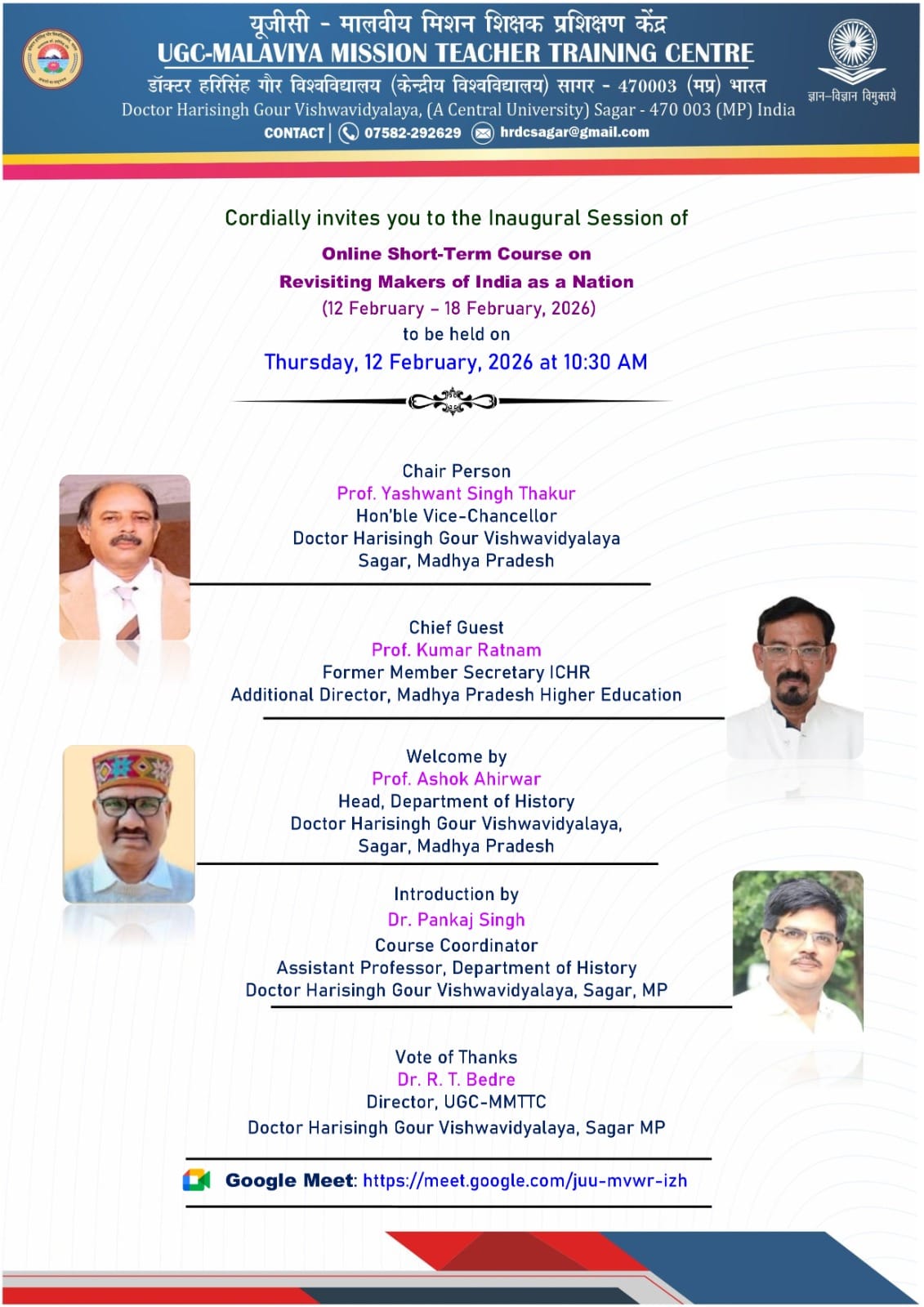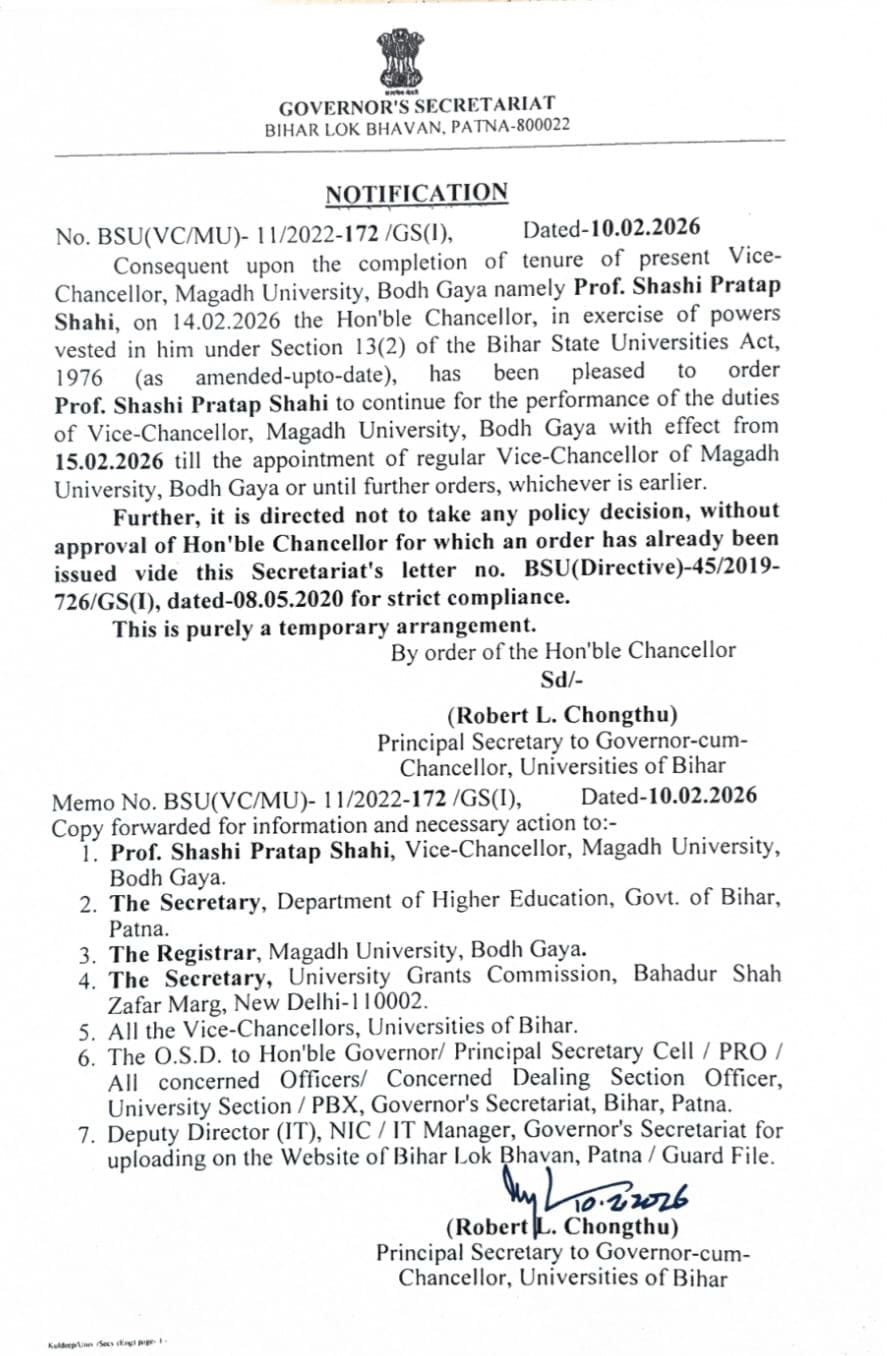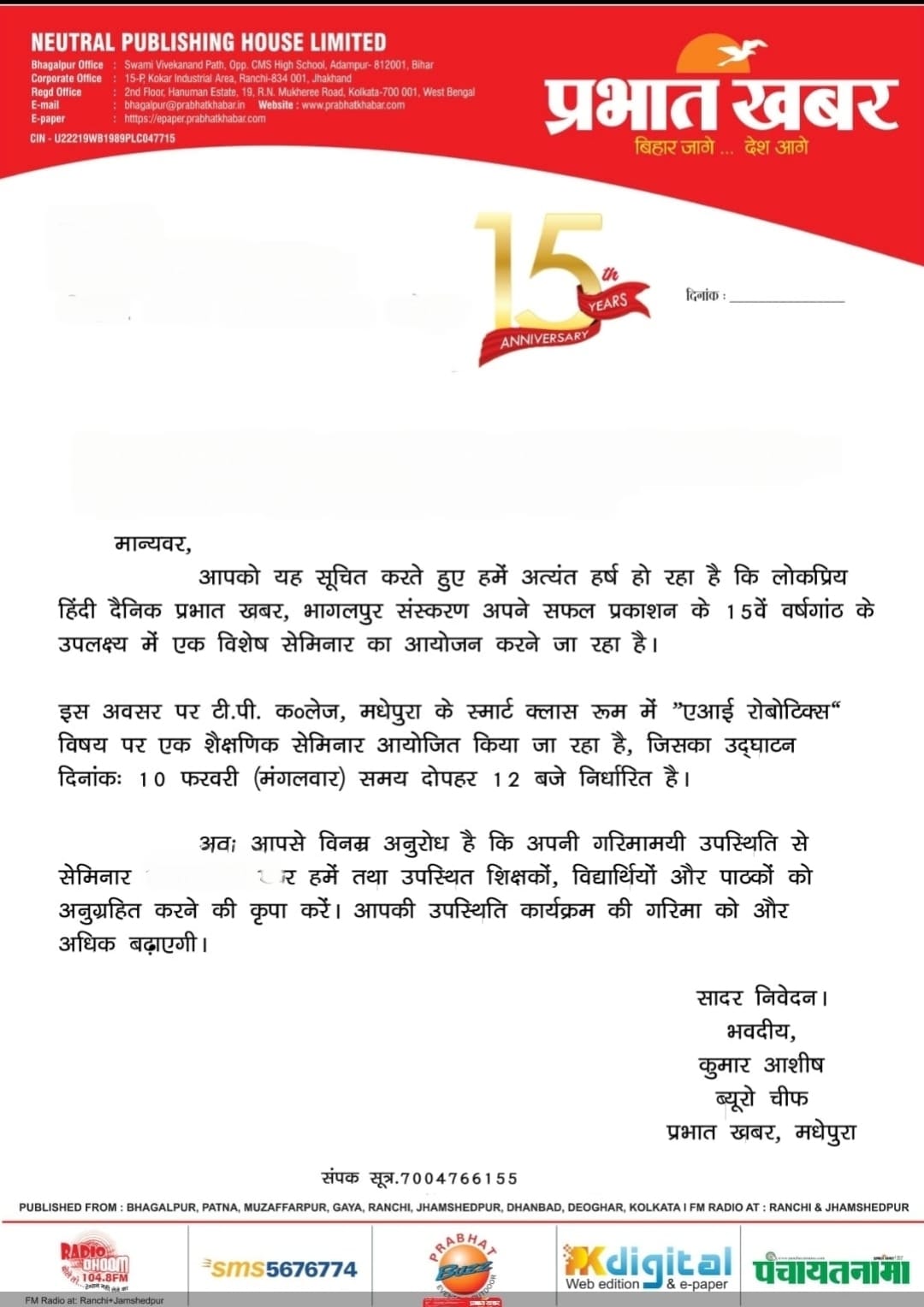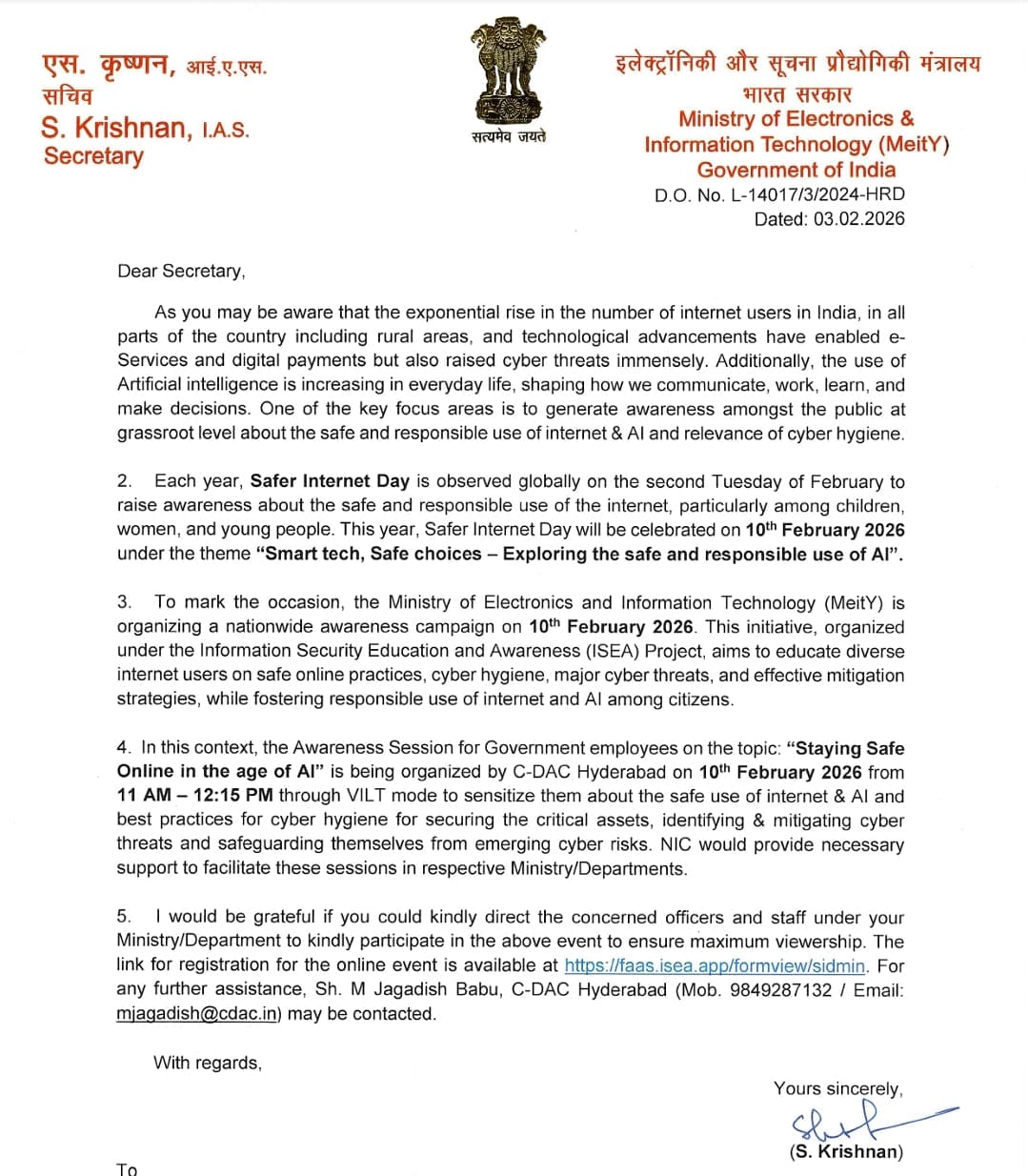विवेकानंद : सार्वभौम धर्म
साधारणतः ‘धर्म’ शब्द से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म आदि का बोध होता है अथवा इन प्रचलित धर्मों के उपासना-स्थलों में जाकर विशेष प्रकार से प्रार्थना या पूजा-पाठ करना धर्म माना जाता है। लेकिन, स्वामी विवेकानंद ‘धर्म’ को इस प्रचलित अर्थ में नहीं लेते हैं। धर्म से मतलब किसी औपचारिक या प्रचलित धर्म से नहीं है, वरन् इससे अभिप्राय उस धर्म से है, जो सभी धर्मों को रेखांकित करता है और जो हमें अपने सृष्टिकर्ता (रचयिता) के सम्मुख खड़ा करता है।“ उनके अनुसार धर्म तत्वमीमांसीय एवं नैतिक जगत के सत्यों से संबद्ध है। धर्म का अर्थ है, एक वैश्विक सत्ता के नैतिक सुशासन में विश्वास। जाहिर है कि उनके लिए धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के संदर्भ के बिना नैतिक जीवन ऐसा ही है, जैसे बालू के आधार पर बना भवन। यदि धर्म को नैतिकता से अलग कर दिया जाए, तो कुछ भी अर्थपूर्ण शेष नहीं रहेगा। धर्म का अर्थ मानव में आध्यात्मिकता का जागरण है और इससे नैतिक मूल्यों को संरक्षण मिलता है। संक्षेप में, धर्म ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ की अभिव्यक्ति है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो धर्मपूर्ण है, वही शुभ है। फिर यदि धर्म मानवता के लिए कल्याणकारी है, तो यह अवश्य ही सुंदर है। अर्थात् अंतःजागरण की एक प्रेरक शक्ति के रूप में धर्म सत्य, शिव और सुंदर में समाहित है।
धर्म आवश्यक एवं अनिवार्य है: धर्म को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। वैसे अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। मगर, माक्र्स आदि कुछ विचारकों को मानने वाले भी बहुत लोग हैं, जिनका विश्वास है कि धर्म अफीम है। ऐसे लोगों के अनुसार मानव जीवन में ‘धर्म’ की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। विवेकानंद का कहना है कि धर्म मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है। मनुष्य सिर्फ रोटी के सहारे नहीं जी सकता। उसमें उच्च वैश्विक सत्ता से संबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है और इसके लिए उसे ‘धर्म’ की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति धर्म के बगैर जीवित नहीं रह सकता। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं, जो अहम् से प्रेरित होकर अपने आपको धर्म से पृथक बताते हैं। वह उस व्यक्ति के समान है, जो कहता है कि वह साँस तो लेता है, लेकिन उसको नाक नहीं है। यहाँ विवेकानंद मानव जीवन में ‘धर्म’ की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। उनका कहना है कि चाहे विवेक से, तर्क से, अंतर्बोध से या अंधविश्वास से, किसी-न-किसी माध्यम से मानव उस दिव्यशक्ति के साथ अपने संबंधों का बोध करता है, यही बोध या अनुभूति ही धर्म है। इस रूप में तथाकथित नास्तिक एवं अधार्मिक व्यक्ति भी वास्तव में धर्मिक ही हैं। यहाँ विवेकानंद यह स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की धर्मिक आस्थाओं एवं अनुभूतियों में परिवर्तनीयता अपरिहार्य है। क्योंकि धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला है। वास्तव में, जितने मस्तिष्क हैं, उतने धर्म भी हो सकते हैं; क्योंकि भगवान की संकल्पना प्रत्येक अपने-अपने ढंग से और विशिष्ट रूप में करता है।
सभी धर्म एक हैं: विवेकानंद ने विश्व के प्रायः सभी धर्मों के मौलिक ग्रंथों का अध्ययन किया और तदुपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म मूलतः एक ही हैं। संसार के सभी धर्मों का सार एक ही है; क्योंकि वे एक ही ईश्वर से उत्पन्न तथा उसी में समाहित होते हैं। उनमें से सभी सत्य को व्यक्त करने वाले हैं; क्योंकि सभी एक ही दैवीय सत्ता से प्रेरित हैं। हिंदुओं के समान ही ईसाई, मुस्लिम तथा पारसियों के पवित्रा ग्रंथ भी देवत्व से प्रेरित हैं। कृष्ण में उतना ही देवत्व है, जितना जीसस एवं मोहम्मद में। ईश्वर एक है, फिर चाहे हम उसे ‘गाॅड’ कहें, ‘खुदा’ कहें या कुछ और कहें, सबका अर्थ एक ही है। हमें मतभिन्नता के आधार पर दूसरों को नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें सत्य के लिए मरने को तत्पर रहना चाहिए। मेरे ख्याल से यही सभी धर्मों का सारतत्व है। सभी धर्म एक ही मूलभूत सत्य को अपनी-अपनी दृष्टि से अभिव्यक्त करते हैं। वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग-अलग मार्ग हैं। उनमें से कोई सत्य तथा कोई असत्य अथवा कोई अधिक सत्य तथा कोई कम सत्य नहीं है। एक सापेक्ष दृष्टि से सभी सत्य हैं और सबों का समान महत्त्व है। इसलिए, अपने धर्म (किसी एक धर्म) को ही एकमात्रा सत्य एवं सर्वश्रेष्ठ बताने की प्रवृति ठीक नहीं है। ‘गाॅड’, ‘अल्लाह’, ‘राम’, ‘नारायण’, ‘ईश्वर’, ‘खुदा’ आदि एक ही रूप के विभिन्न स्वरूप हैं। ईश्वर की कृपा पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता चाहे वे कोई भी धर्म, जाति, नस्ल या देश के हों। वास्तव में, शुभ प्रत्येक धर्म की नींव में है, और प्रत्येक धर्म अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं में उस समय तक अच्छा रहता है, जबतक उसे हठधर्मिता एवं जड़ता, दोनों से मुक्त रखा जाता है। अतः, हमें दूसरे धर्मों के प्रति अपनी सोच में कभी आलोचक या निंदक का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमारा लक्ष्य अन्य धर्मों के श्रेष्ठतम् गुणों को प्राप्त कर उसका इस्तेमाल संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए करना होना चाहिए।
वास्तव में, विभिन्न धर्मों में कोई मौलिक विरोध नहीं है। कोई किसी दूसरे का खंडन नहीं करता, बल्कि प्रत्येक धर्म में अन्य धर्मों के विचारों की पुष्टि ही होती है। हर धर्म एक.दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। धर्म का केंद्र जो ‘सत्य’ है, वह इतना व्यापक है कि एक साथ उसके सभी पक्षों पर विचार करना मुश्किल है। हर धर्म उसी ‘सत्य’ के किसी पक्ष या पहलु की व्याख्या करता है और भावातिरेक में यह समझ बैठता है कि ‘सत्य’ में मात्रा वही एक पक्ष है, जो उसे दृष्टिगोचर हो रहा है।
‘सार्वभौम धर्म’ का अर्थ: विवेकानंद के पूर्व भी भारत एवं दुनिया के कई अन्य विचारकों ने ‘सार्वभौम धर्म’ की कल्पना की है और विभिन्न धर्मों को एकसूत्रा में पिरोने की कई कोशिशें हुई हैं। लेकिन, सामान्यतः ये कल्पनााएँ एवं कोशिशें साकार एवं यथार्थ रूप ग्रहण नहीं कर पायी हैं। विवेकानंद ने इसके दो कारण माने हैं। एक, पूर्व में सार्वभौम धर्म के लिए किसी व्यावहारिक प्रणाली का अवलंबन नहीं किया गया। दूसरा, पूर्व में यह तो स्वीकार किया गया कि संसार के सभी धर्म सत्य हैं, लेकिन उनको समन्वित करने का कोई वैसा उपाय नहीं किया गया, जिससे विभिन्न धर्मों की विशिष्टता सुरक्षित रह सके।
‘सार्वभौम धर्म’ का अर्थ विभिन्न धर्मों के योग का संश्लेषण नहीं है। वास्तव में बिना विशेष के सार्वभौम एक अमूर्त एवं निरर्थक विचार है और तद्नुरूप सार्वभौम धर्म भी बिना विशिष्ट धर्म के एक अमूर्त एवं निरर्थक धारणा बन जाएगा। ‘सार्वभौम धर्म’ का यह अर्थ भी नहीं है कि एक प्रकार के विशेष मत में विश्व के सभी व्यक्ति विश्वास करें और उसे ही अपना धर्म मानें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में धर्म का एक ही प्रचलित रूप नहीं हो सकता है और न ही कोई एक अनुष्ठान पद्धति सर्वमान्य हो सकती है।2
वास्तव में, विभिन्नता एवं वैषम्यता ही जीवन एवं चिंतन की उन्नति का मार्ग है। यदि संपूर्ण एकरूपता एवं साम्यता आ जाए, तो विकास अवरूद्ध हो जाएगा।
विवेकानंद के अनुसार, धर्म व्यक्ति में कहीं बाहर से नहीं आता है, वरन् व्यक्ति के अभ्यंतर से ही उदित होता है।3 धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सन्निहित है। जबतक मनुष्य का शरीर, मन, मस्तिष्क एवं जीवन है, मनुष्य चाहकर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। जबतक मनुष्य में सोचने की शक्ति है, तबतक किसी न किसी रूप में धर्म का अस्तित्व रहेगा।4
विवेकानंद यह स्वीकार करते हैं कि विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच मत-मतांतर, वाद-विवाद, झगड़े एवं युद्ध हुए हैं। लेकिन, यह सब धर्म के मूल मर्म को नहीं समझने अथवा गलत रूप में समझने के कारण है। वास्तव में, धर्म ने सर्वापेक्षा अधिक प्रेम, भ्रातृत्व एवं शांति का विस्तार किया है और मानव जीवन को बेहतर बनाने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, प्रत्येक धर्म में महान सार्वभौमिक तत्त्व होता है, जिसके कारण धर्म वर्जना का नहीं योगदान का विषय है।¬5 यही कारण है कि अति प्राचीन काल से ही कुछ धर्म विभिन्न धर्मों की विवधता को बचाये-बनाये रखने के पक्षधर रहे हैं। सभी धर्मों में जगत के कल्याण का एक महानभाव और शुभद्देश्य निहित है। ऐसे में किसी भी धर्म को विनष्ट करना उचित नहीं है।6
‘सार्वभौम धर्म’ के अनिवार्य लक्षण: विवेकानंद के अनुसार ‘सार्वभौम धर्म’ की सार्वभौमता मूलतः दो अनिवार्य लक्षणों पर आधृत है। एक, कोई भी धर्म तभी सार्वभौम हो सकता है, जब इसका द्वार सबों के लिए खुला रहे। दरअसल, नवजात शिशु अबोध तथा निर्दोष होता है, वह किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। यह बात दीगर है कि सामान्यतः बच्चा अपने माँ-बाप का ही धर्म स्वीकारता है। ऐसा इसलिए होता है; क्योंकि बचपन से ही उसका सामाजिक परिवेश एवं उसकी शिक्षा-दीक्षा उसे माँ-बाप के धर्म की ओर ही उन्मुख कर देती है।
दूसरा, ‘सार्वभौम धर्म’ में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके। दरअसल, धर्मों को लेकर विभिन्न संस्थाओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है और उनके आपसी मतभेदों एवं विवादों का पूर्ण शमण भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में ‘सार्वभौम धर्म’ से यह अपेक्षा है कि वह सभी धर्मों को साथ लेकर चले और उसमें सभी धर्म संस्थाओं को ‘सार’ या ‘सार्थकता’ दिखायी दे।
‘सार्वभौम धर्म’ है: विवेकानंद का कहना है कि उक्त दोनों शर्तों का पालन करने वाले ‘सार्वभौम धर्म’ की संभावना पर संशय करना या उसकी संभावना पर प्रश्न उठाना अकारण है; क्योंकि ऐसा ‘सार्वभौम धर्म’ वस्तुतः ‘है’। उनके अनुसार, जिस प्रकार विश्वबंधुत्व एक तात्त्विक तथ्य है एवं मानवमात्रा में एक मौलिक एकता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों को उसकी चेतना नहीं है। उसी प्रकार ‘सार्वभौम धर्म’ भी एक वास्तविकता है, भले ही विभिन्न धर्मावलंबियों को उसकी अवगति न हो। इसलिए, ‘सार्वभौम धर्म’ को मानने का अर्थ अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य (सार्वभौम) धर्म को मानना नहीं है। हम चाहे जिस किसी भी प्रचलित धर्म को अंगिकार करें, हम ‘सार्वभौम धर्म’ को ही अंगीकार करेंगे। क्योंकि वस्तुतः हर धर्म ‘सार्वभौम धर्म’ है, लेकिन हम अपनी सुविधा एवं बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस धर्म की सार्वभौमिकता की उपेक्षाकर उसे सांप्रदायिक बना देते हैं।
‘सार्वभौम धर्म’ के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म का पालन खुले हृदय से करें। हम समझें कि मेरे लिए जो मार्ग है, वह सत्य है, लेकिन अन्य अनेकों मार्ग भी हो सकते हैं।
‘सार्वभौम धर्म’ का मूलमंत्रा: ‘सर्वभौम धर्म’ का मूलमंत्रा ‘स्वीकृति’ है। यहाँ ‘स्वीकृति’ और ‘सहिष्णुता’ में भेद करना आवश्यक है। ‘सहिष्णुता’, एक अभावात्मक अवधारणा है, जो ‘सहन करने’ एवं ‘बदार्शत करने’ की बात करता है। लेकिन, ‘स्वीकृति’ एक भावात्मक अवधारणा है, जो दूसरे मार्ग को भी अपने मार्ग की तरह ही सत्य मानता है और उससे भी कोई उपयोगी सीख मिले, तो उसे ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। जाहिर है कि ‘सार्वभौम धर्म’ में यह भी विशिष्टता होनी चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को सहजरूप से स्वीकार्य हो। इसके लिए उसमें दर्शन, भावना, कर्म एवं रहस्यवादिता-सभी के लिए स्थान होना जरूरी है, ताकि वह विभिन्न मनोवृत्तियों वाले मनुष्यों की भावनाओं को संतुष्ट कर सके। इसी दृष्टि से भारतीय विचारकों ने यौगिक एकत्व पर बल दिया है। कर्ममार्गी के लिए यह मानवमात्रा का एकत्व है, रहस्यात्मक वृत्ति वालों केलिए यह निम्नतर आत्मा एवं उच्चतर आत्मा का एकत्व है, भक्तिमार्गी के लिए यह भक्त एवं भगवान का एकत्व है और ज्ञानमार्गी के लिए यह एक ही परमसत् की अनुभूति है।
निष्कर्ष: वर्तमान संदर्भ में धर्म का नाम काफी बदनाम हो गया है। वैसे धर्म के ठेकेदारों ने पहले से ही इसे अंधविश्वास एवं ठगी को बढ़ावा देने का जरिया बना रखा था। लेकिन, आजकल धर्म की आड़ में आतंकवाद एवं सांप्रदायिक दंगे भड़काने की प्रवृत्ति भी बढ़ गयी है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर झगड़े बढ़े हैं। प्रायः सभी धर्मों में अपने आपको सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। इस सब की जड़ में है, धर्मिक शिक्षाओं की गलत समझ एवं व्याख्या। इसलिए, हमें यह समझना होगा कि सभी धर्म मानव एवं मानवता की भलाई के लिए हैं। इस दृष्टि से सभी एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं। ऐसे में, यह आवश्यक हो जाता है कि हम दूसरों की आस्थाओं एवं विश्वासों को भी स्वीकार करें। दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। इसतरह की स्वीकार्यता, सहिष्णुता एवं समभाव की भावना से ही न्याय, शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिशा में हम विवेकानंद के ‘सार्वभौम धर्म’ संबंधी विचारों से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं।
संदर्भ
1. विवेकानंद, स्वामी; विवेकानंद साहित्य, खंड-प्प्ए अद्वैत आश्रम, कोलकाता
(पश्चिम बंगाल).
2. वही, खंड-प्प्प्ए पृ. 145.
3. वही, खंड-प्ट, पृ. 187.
4. वही.
5. वही, पृ. 130-138.
6. वही, पृ. 125-131.
-सुधांशु शेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, मधेपुरा, बिहार