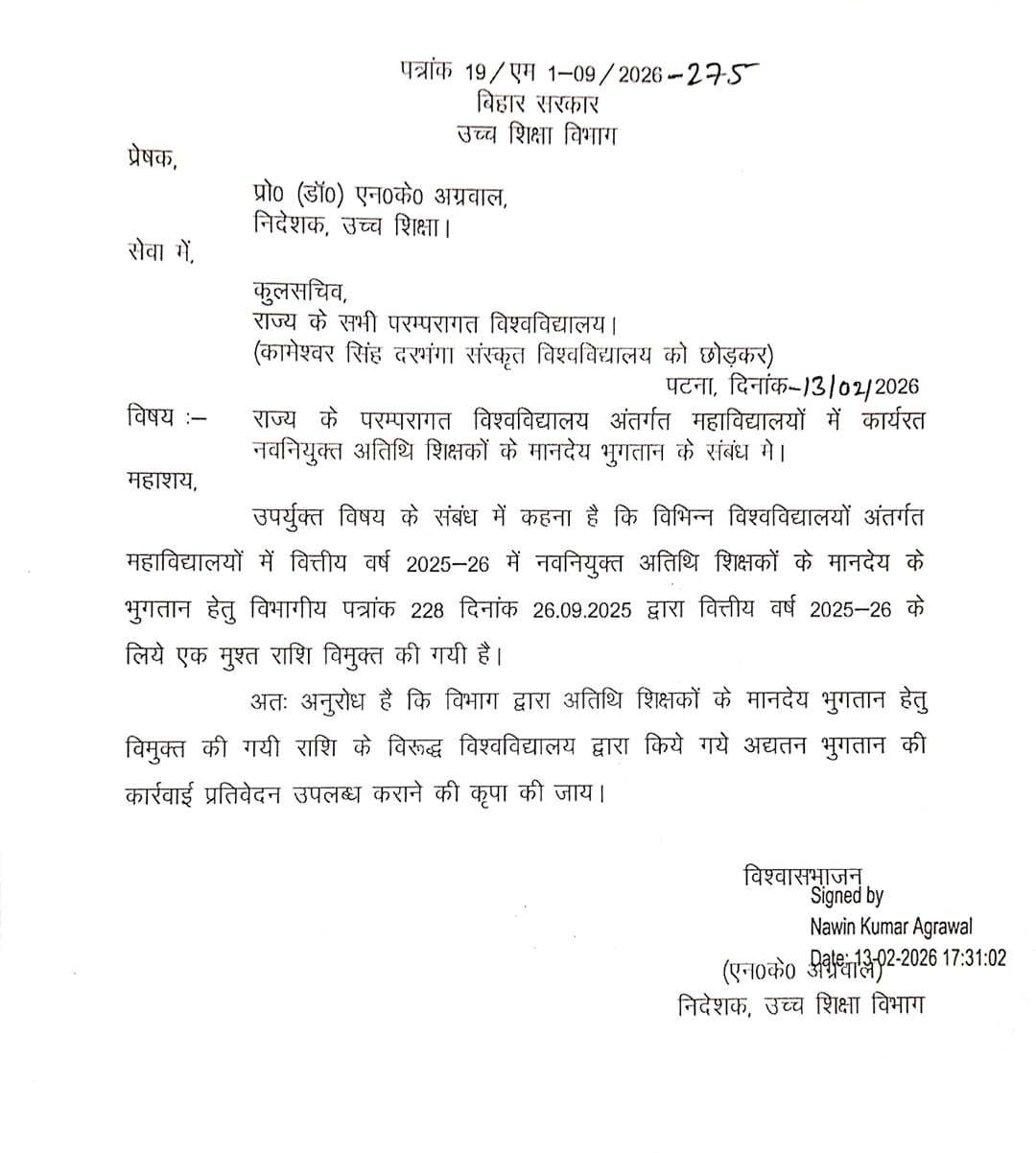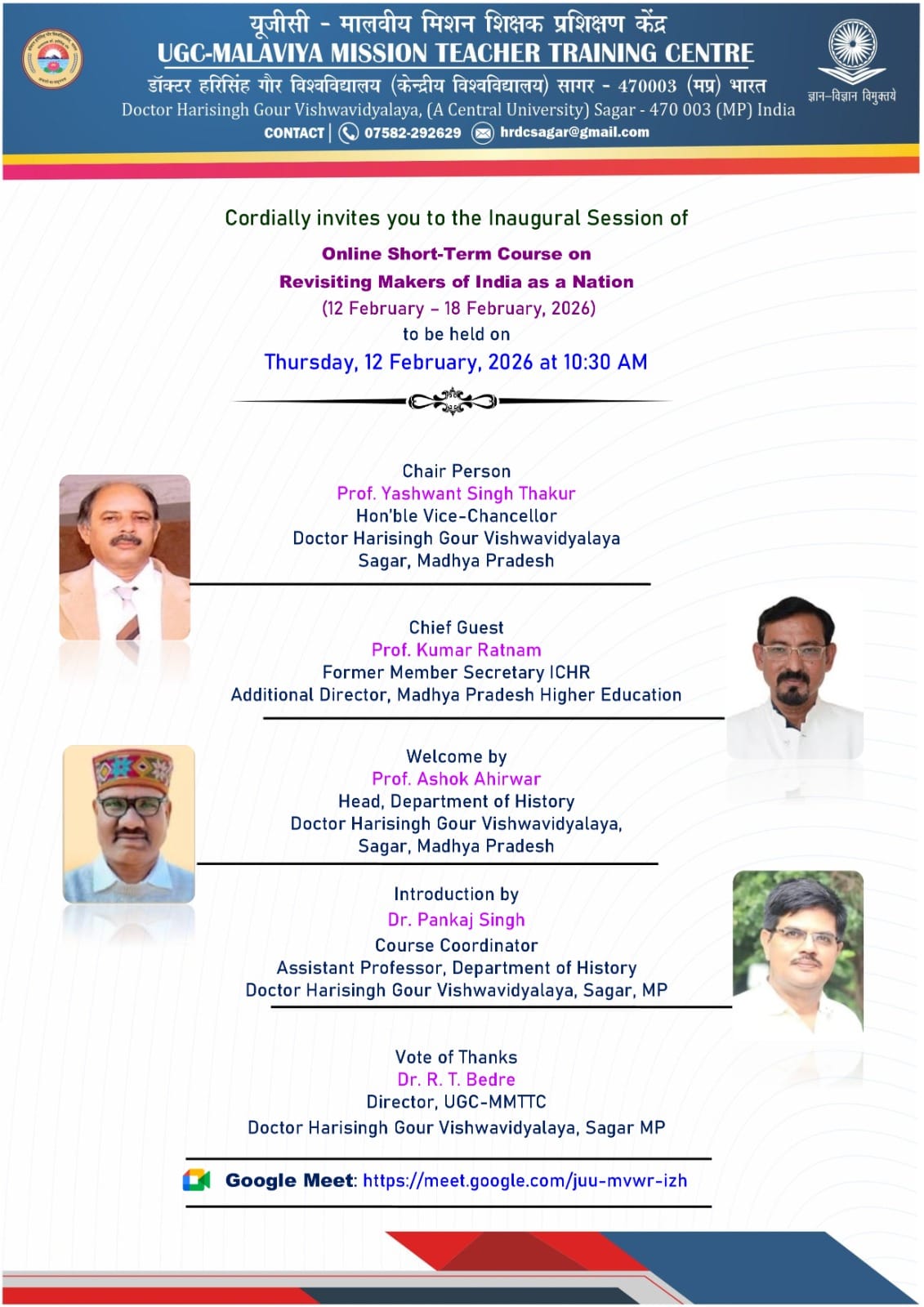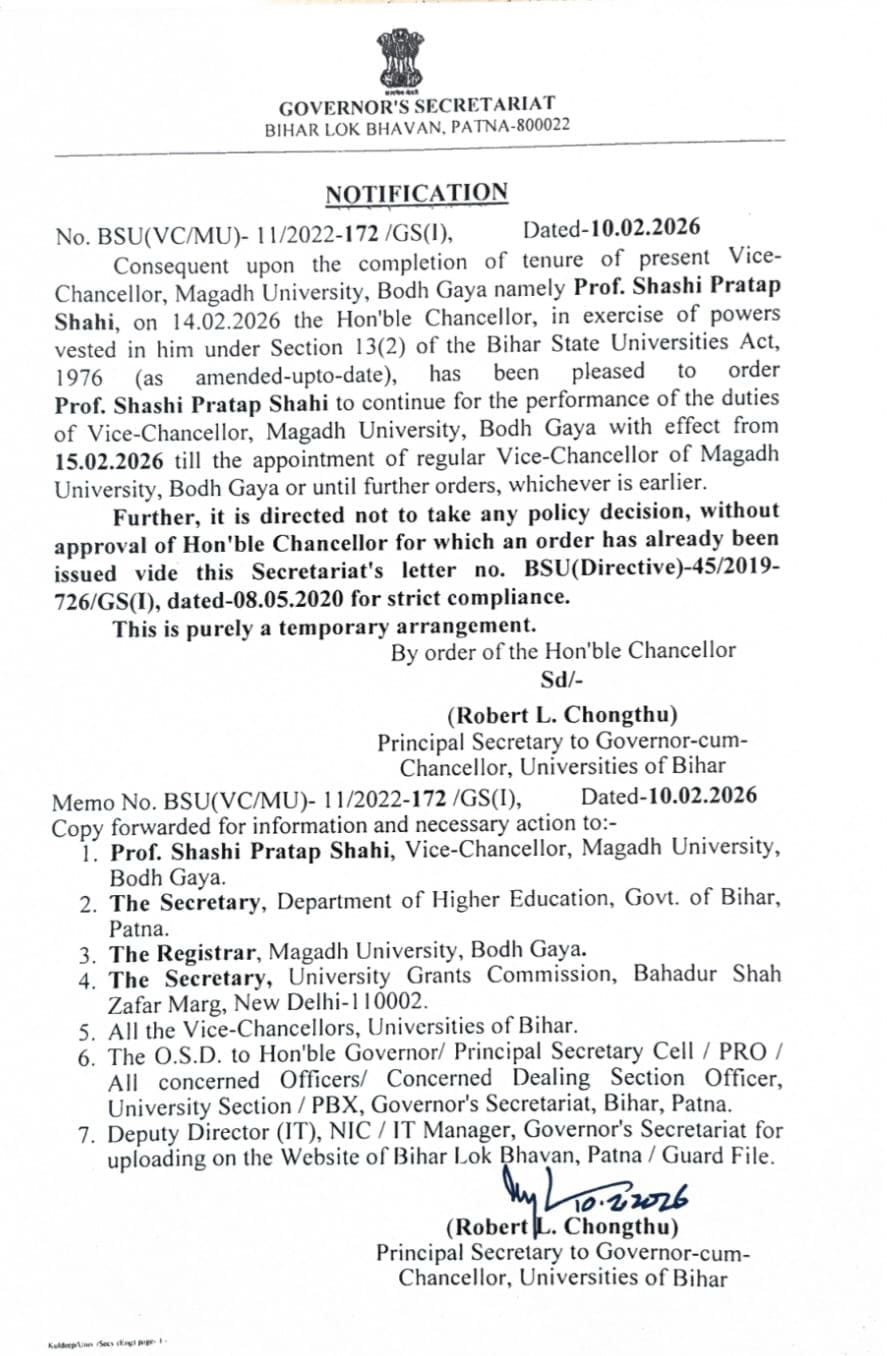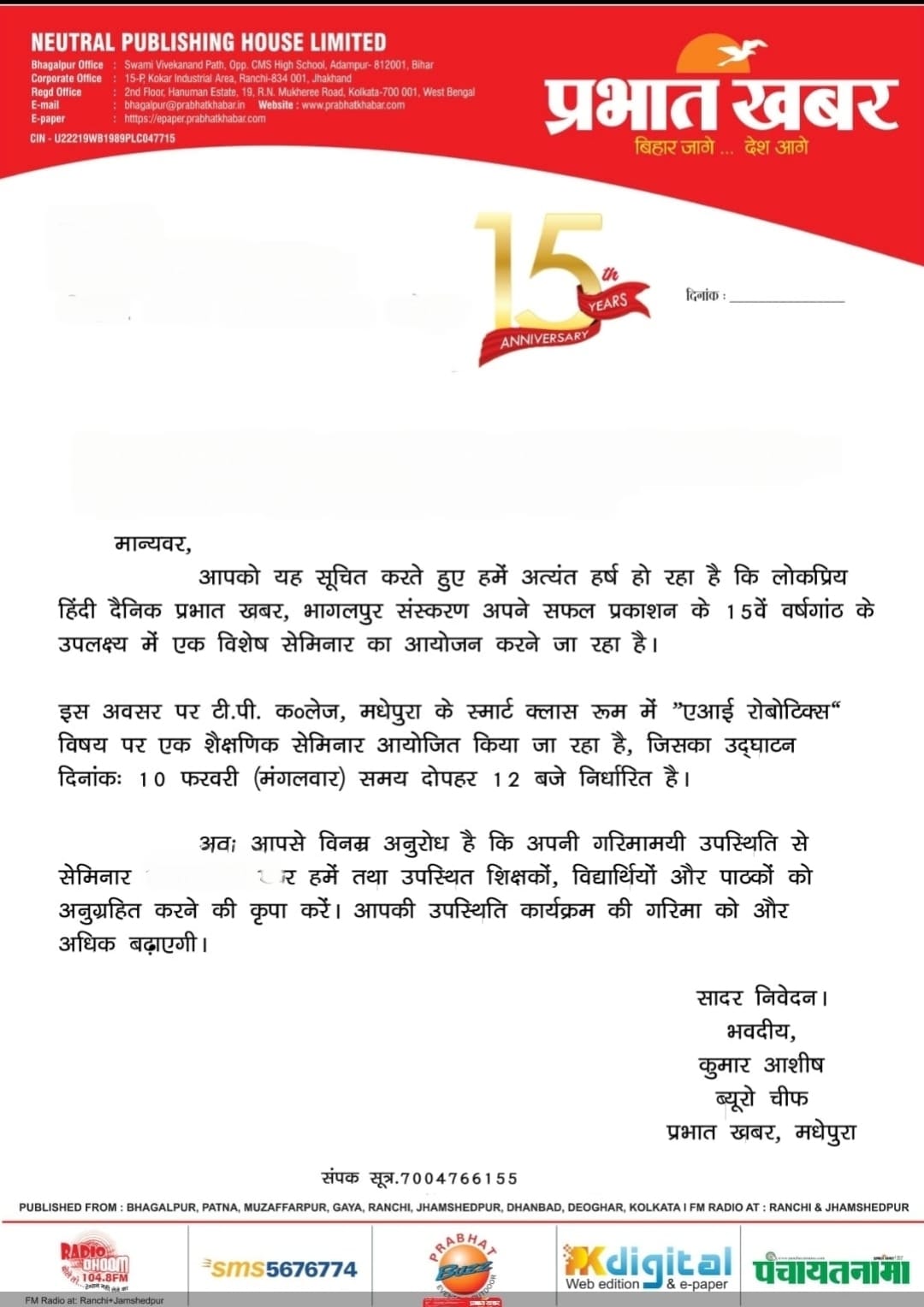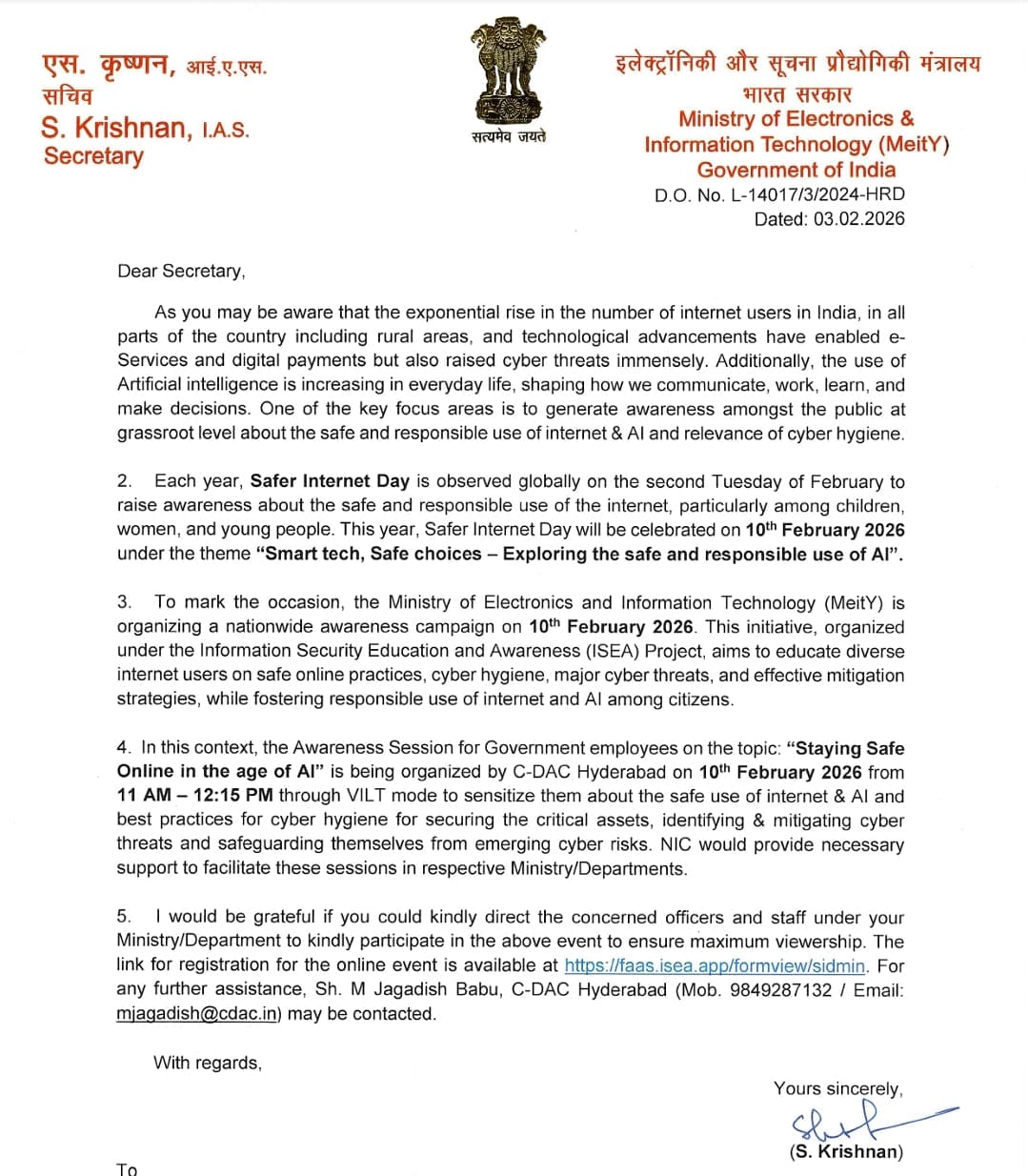तदुपरान्त बनाम तदोपरान्त
मेरे प्राध्यापकीय जीवन के प्रारम्भिक दिन थे। उनदिनों मैं भागलपुर के टी.एन.बी. काॅलेज में पदस्थापित था। बी. ए. के पाठ्यक्रम में हिन्दी की एक पुस्तक लगी थी, जिसका सम्पादन स्थानीय वरिष्ठ प्राध्यापक ने किया था। उस पुस्तक की भूमिका के अतिरिक्त हर पाठ के पूर्व लिखित कवि/लेखक-परिचय में कम-से-कम डेढ़ दर्जन स्थलों पर सम्पादक महोदय ने ‘तदुपरान्त’ की जगह ‘तदोपरान्त’ का प्रयोग कर रखा था। यह मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी; क्योंकि अर्थ की दृष्टि से दोनों में स्प ष्ट अन्तर है। चलिए, दोनों के बीच का तात्त्विक अन्तर समझें।
तत्+उपरान्त = तदुपरान्त (व्यंजन सन्धि) का शाब्दिक अर्थ होता है– उसके बाद (आफ़्टर दैट)। आपने ‘तत्’ (वह ) शब्द रूप पढ़ा होगा। पुलिंग में सः (एकवचन)- तौ (द्विवचन)-ते (बहुवचन) स्त्रीलिंग में सा (एक वचन)-ते ( द्विवचन)-ताः(बहुवचन) तथा नपुंसक लिंग में तत्(एकवचन)-ते(द्विवचन)-तानि(बहुवचन) रूप बनते हैं। तत्(सर्वनाम) का सामान्यावस्था में अर्थ होता है- वह ( दैट)। यहाँ इसका अर्थ होगा ‘उसके’ तथा उपरान्त का बाद/पश्चात्/तदनु/तदनन्तर। ज्ञातव्य है कि ‘उपरान्त’ ऊर्ध्व -> उप (आदेश) +रिल् -> रि = उपरि+अन्त = उपर्यन्त (इको यणचि) का तद्भव-रूप है, जिसका विकास-क्रम यों बनेगा- उपर्यन्त > > उपरन्त > उपरान्त (मुख-सुख से)।
अब प्रश्न उठता है कि ‘तत्’ का ‘त्’ ‘द्’ में कैसे परिणत हुआ? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको महावैयाकरण पाणिनि के पास लिये चलता हूँ। उनकी विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘अष्टाध्यायी’ के ‘हल्सन्धिप्रकरणम्’ में एक सूत्र प्रयुक्त हुआ है- ‘झलां जशोऽन्ते’ (8/2/39), पदान्ते झलां जशः स्युः । वागीशः। अर्थात् ‘झल्’ प्रत्याहार के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा श्, ष्, ह् ‘जश्’ प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्गों के तृतीय वर्ण- ज्, ब्, ग्, ड्, द् आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए वाक् -> वाग्+ईशः = वागीशः। ध्यातव्य है कि ये आदेश ‘स्थानेऽन्तरतमः’ परिभाषा के अन्तर्गत होते हैं। आदेश की प्रायोगिक प्रक्रिया अधोलिखित सारणी में द्रष्टव्य है–
झल् जश् साम्य-स्थान
1. झ्, ज्, छ्, च्, श् ज् तालु
2. भ्, ब्, फ्, प् ब् ओष्ठ
3. घ्, ग्, ख्, क्, ह् ग् कण्ठ
4. ढ्, ड्, ठ्, ट्, ष् ड् मूर्धा
5. ध्, द्, थ्, त्, स् द् दन्त
चूँकि, तवर्गीय ध्वनियों का उच्चारण ‘दन्त’ से होता है, फलस्वरूप् ये ‘दन्त्य’ कहलाती हैं। ‘त्’ और ‘द्’ – दोनों तवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। यही कारण है कि ‘झल्’ प्रत्याहार का सदस्य ‘त्’ जश् के तृतीय वर्ण में परिणत होकर ‘द्’ बना। पुनः, ‘उपरान्त’ के ‘उ’ के साथ मिलकर ‘दु’ बन गया। इसतरह, तत् -> तद् +उपरान्त = तदुपरान्त की निर्माण-प्रक्रिया पूरी होती है।
अब ‘तदोपरान्त’ शब्द पर विचार किया जाए। तदा + उपरान्त = तदोपरान्त का शाब्दिक अर्थ होता है– तब या उस समय के बाद। ‘तदा’ संस्कृत का बहुप्रचलित अव्यय है, जिसका अर्थ होता है – तस्मिन् काले, अर्थात् तब/उस समय। श्रीमद्भगवद्गीता का प्रसिद्ध श्लोक है–
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
अर्थात् जब-जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब(-तब) मैं अवतार लेता हूँ।
इस श्लोक में यदा (जब) के साथ ‘तदा’ (तब) का प्रयोग हुआ है। यहाँ यह कालबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त है।
इसीतरह, ‘तदोपरान्त’ का ‘तदा’ भी कालबोधक क्रियाविशेषण’ या अव्यय है। इसका रूप सदैव एक-सा बना रहता है, इसीलिए इसे अव्यय कहते हैं। ‘तदा’ और ‘तदुपरान्त’ व्यावहारिक दृष्टि से लगभग समान भाव रखते हैं । आप ‘तदा’ कहिए या तदुपरान्त। ‘तदोपरान्त’ कहना अथवा लिखना तो कहीं से भी उचित नहीं है। यही कारण है कि ‘तदुपरान्त’ के स्थान पर ‘तदोपरान्त’ का प्रयोग सर्वथा निन्दनीय माना गया है।

बहादुर मिश्र
1/8/2020