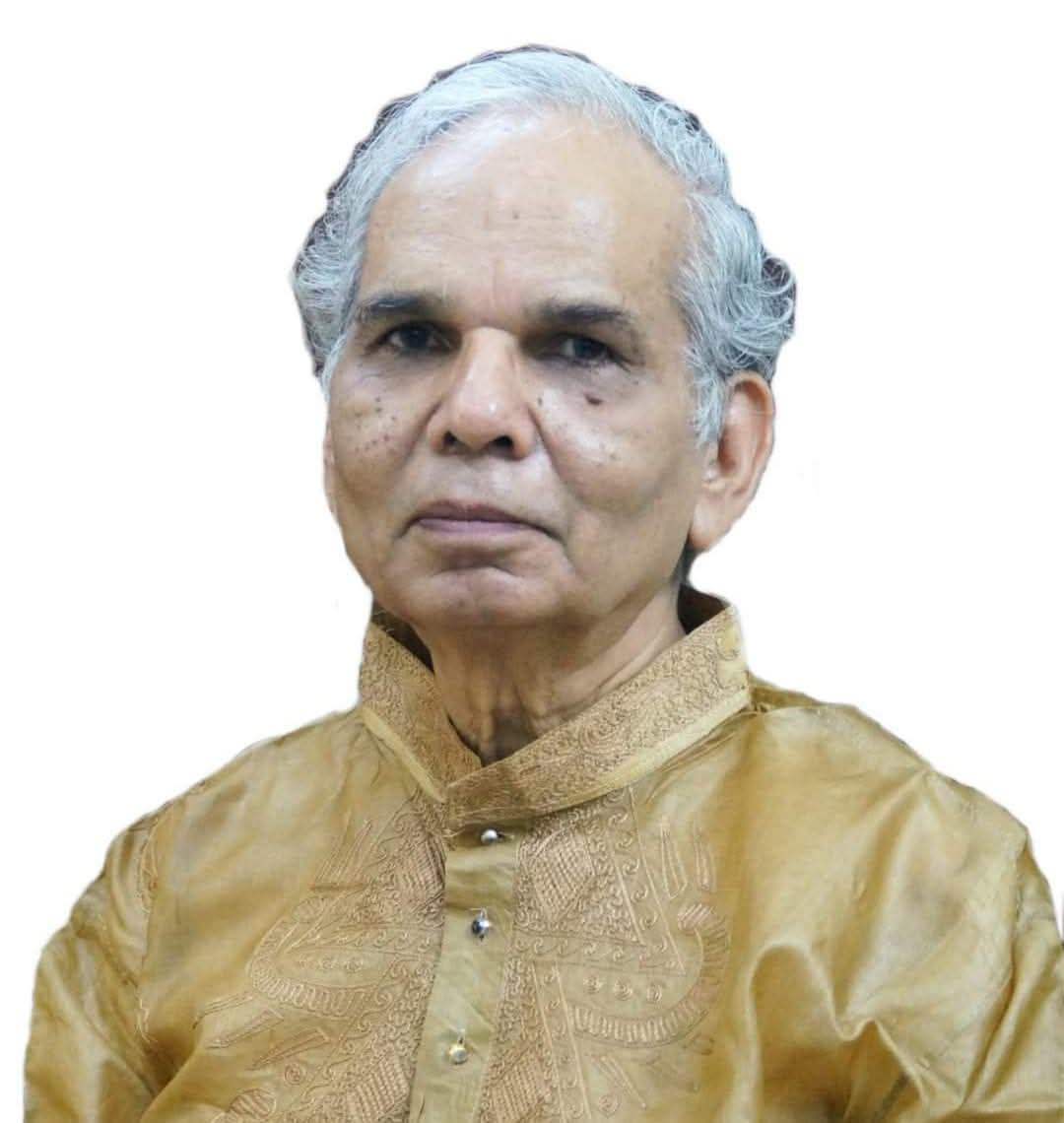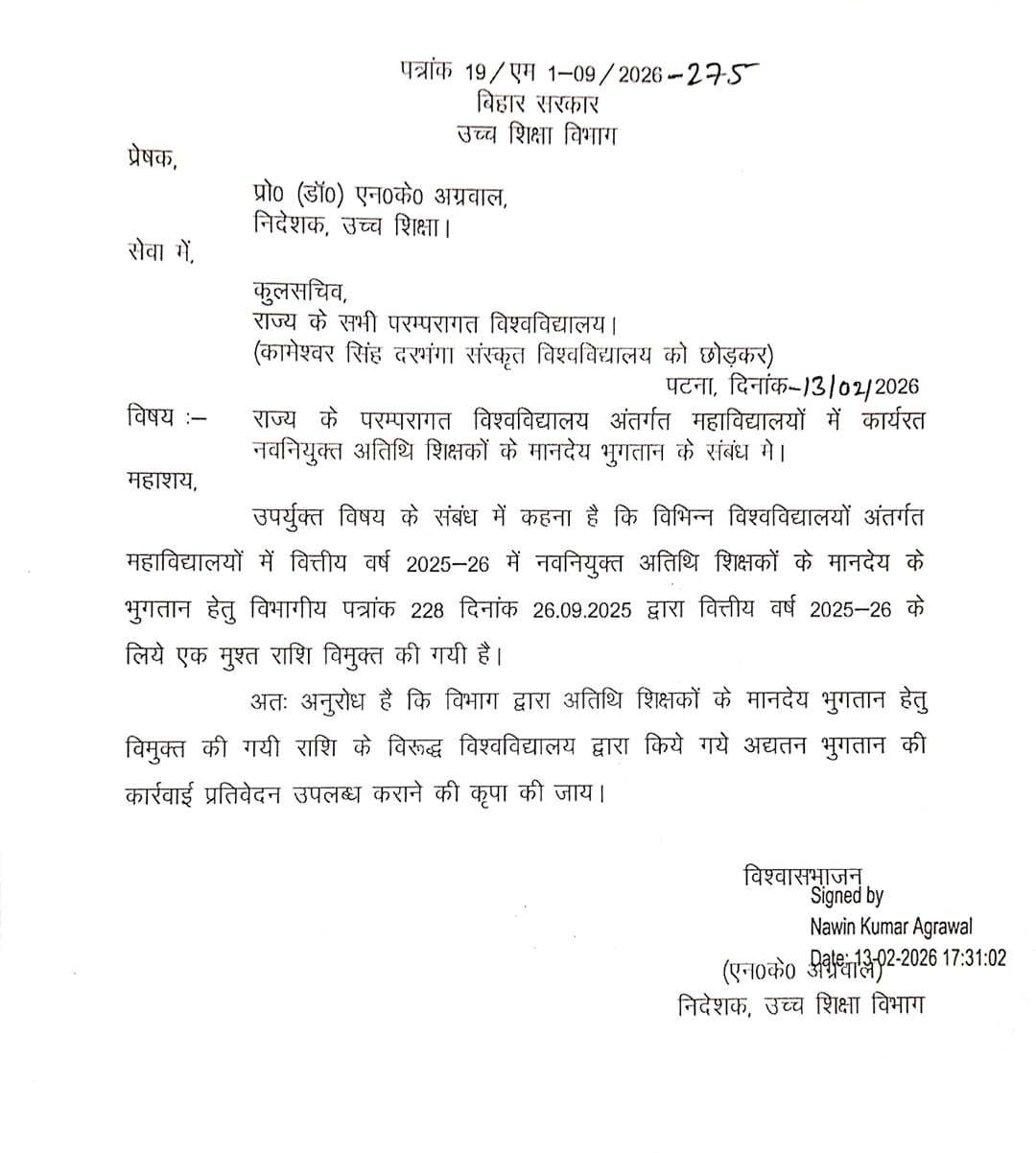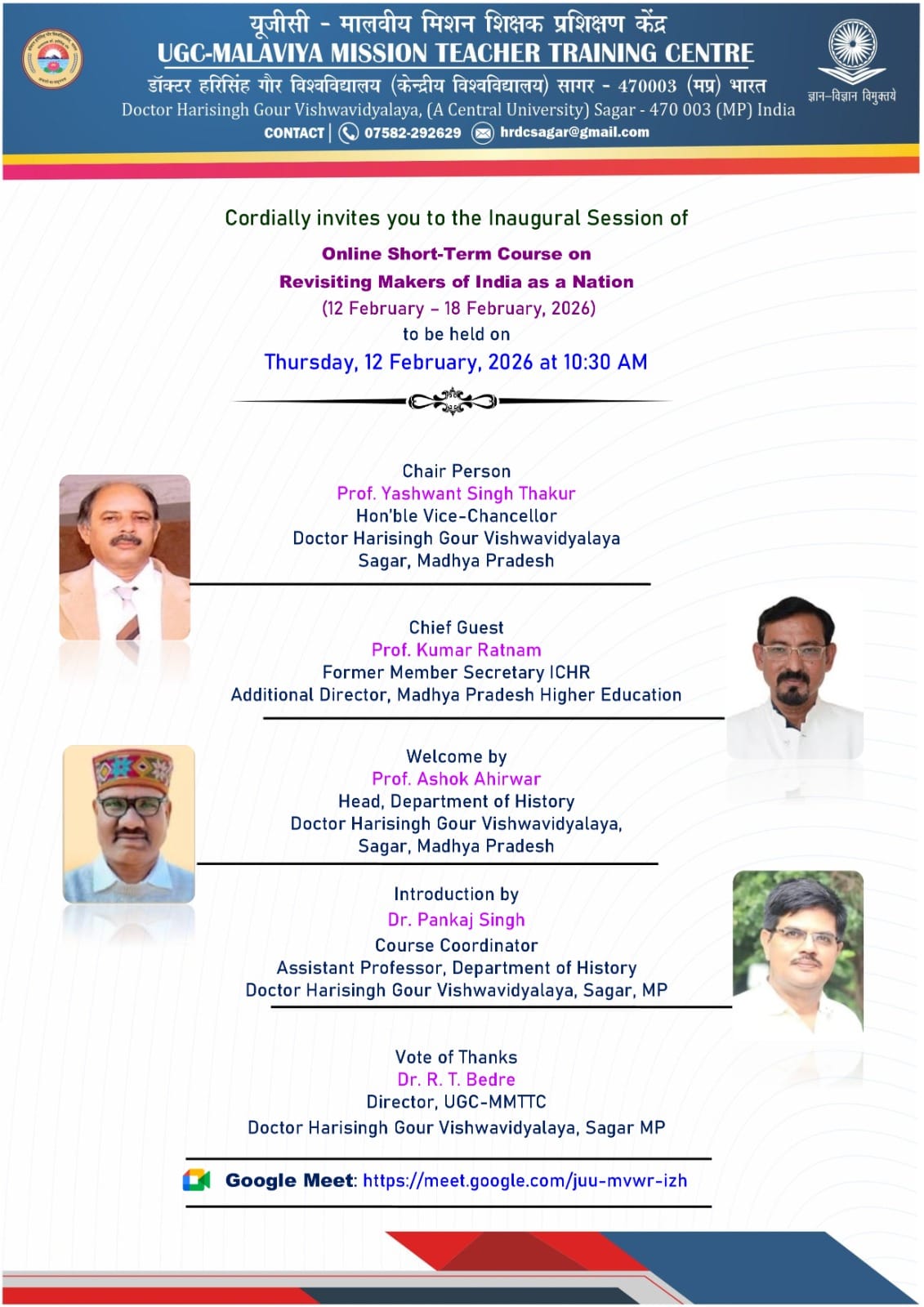*शोध में नैतिक मूल्यों का पालन अनिवार्य।*
*अच्छे शोध कार्य के लिए शोधार्थियों का ईमानदार होना आवश्यक।*
*सभी विश्वविद्यलयों और संस्थानों को नैतिकता अपनानी होगी।*
*प्रो डॉ धर्मेन्द्र कुमार सिंह*
*शोध प्रारूप तैयार करना एक कला*
*शोधार्थी शोध प्रणाली पर दें ध्यान।*
*व्यज्ञानीक शोध के लिए व्यज्ञाणिक पद्धति अपनाएं शोधार्थी।*
*प्रो डॉ दिनेश कुमार*

शोध कौशल पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला के चौथे दिन स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में दो सत्रों में शोधार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
पहले सत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, गया के प्रोफेसर डॉ धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष एवम् स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंस के डीन ने शोध में नैतिक मूल्यों पर शोधरथियों के सामने नैतिकता, ईमानदारी और पर विस्तपुर्वक बातें रखीं। वह आयोजित कार्यशाला में ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने बताया कि शोध की नैतिकता सदैव ही संदेह से परे होनी चाहिये। शोध में नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली का अधिकांशतः नकल करते हुये अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी है ।नैतिकता’ को परिभाषित करने का एक अन्य तरीका उन विषयों पर केंद्रित है जो आचरण के मानकों का अध्ययन करते हैं, जैसे दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। उदाहरण के लिए, एक “चिकित्सा नीतिशास्त्री” वह व्यक्ति होता है जो चिकित्सा में नैतिक मानकों का अध्ययन करता है। कोई नैतिकता को कार्य करने का तरीका तय करने और जटिल समस्याओं और मुद्दों का विश्लेषण करने की एक विधि, प्रक्रिया या परिप्रेक्ष्य के रूप में भी परिभाषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जटिल मुद्दे पर विचार करते समय , कोई व्यक्ति समस्या पर आर्थिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक या नैतिक दृष्टिकोण अपना सकता है। जबकि एक अर्थशास्त्री ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विभिन्न नीतियों की लागत और लाभों की जांच कर सकता है, एक पर्यावरण नैतिकतावादी दांव पर लगे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की जांच कर सकता है।कई अलग-अलग विषयों, संस्थानों और व्यवसायों में व्यवहार के मानक होते हैं जो उनके विशेष उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। ये मानक अनुशासन के सदस्यों को उनके कार्यों या गतिविधियों का समन्वय करने और अनुशासन के प्रति जनता का विश्वास स्थापित करने में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, नैतिक मानक चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग और व्यवसाय में आचरण को नियंत्रित करते हैं। नैतिक मानदंड अनुसंधान के उद्देश्यों या लक्ष्यों को भी पूरा करते हैं और उन लोगों पर लागू होते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्य विद्वतापूर्ण या रचनात्मक गतिविधियाँ करते हैं। यहां तक कि एक विशेष अनुशासन, अनुसंधान नैतिकता भी है, जो इन मानदंडों का अध्ययन करता है।ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से शोध में नैतिक मानदंडों का पालन करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, मानदंड अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं , जैसे ज्ञान, सत्य और त्रुटि से बचाव। उदाहरण के लिए, शोध डेटा को गढ़ने , गलत साबित करने या गलत तरीके से पेश करने पर प्रतिबंध सच्चाई को बढ़ावा देता है और त्रुटि को कम करता है।कई अलग-अलग लोगों के बीच सहयोग और समन्वय शामिल होता है, नैतिक मानक उन मूल्यों को बढ़ावा देते हैं जो सहयोगात्मक कार्य के लिए आवश्यक हैं , जैसे विश्वास, जवाबदेही, पारस्परिक सम्मान और निष्पक्षता। उदाहरण के लिए, अनुसंधान में कई नैतिक मानदंड, जैसे लेखकत्व के लिए दिशानिर्देश , कॉपीराइट और पेटेंटिंग नीतियां , डेटा साझाकरण नीतियां और सहकर्मी समीक्षा में गोपनीयता नियम, सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए बौद्धिक संपदा हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अधिकांश शोधकर्ता अपने योगदान के लिए श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनके विचार चोरी हो जाएं या समय से पहले प्रकट न हो जाएं।कई नैतिक मानदंड यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि शोधकर्ताओं को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सकता है । उदाहरण के लिए, अनुसंधान कदाचार, हितों के टकराव, मानव विषयों की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल और उपयोग पर संघीय नीतियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सार्वजनिक धन से वित्त पोषित शोधकर्ताओं को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके।अनुसंधान में नैतिक मानदंड भी अनुसंधान के लिए सार्वजनिक समर्थन बनाने में मदद करते हैं। अगर लोग शोध की गुणवत्ता और अखंडता पर भरोसा कर सकते हैं तो उनके शोध परियोजना को वित्त पोषित करने की अधिक संभावना है।अनुसंधान के कई मानदंड कई अन्य महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं , जैसे सामाजिक जिम्मेदारी, मानवाधिकार, पशु कल्याण, कानून का अनुपालन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। अनुसंधान में नैतिक चूक मानव और पशु विषयों, छात्रों और जनता को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता जो नैदानिक परीक्षण में डेटा तैयार करता है, वह मरीजों को नुकसान पहुंचा सकता है या मार भी सकता है, और एक शोधकर्ता जो विकिरण या जैविक सुरक्षा से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, वह अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा या कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और छात्र अनुसंधान के संचालन के लिए नैतिकता के महत्व को देखते हुए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई अलग-अलग पेशेवर संघों, सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान नैतिकता से संबंधित विशिष्ट कोड, नियम और नीतियां अपनाई हैं। कई सरकारी एजेंसियों के पास वित्त पोषित शोधकर्ताओं के लिए नैतिक नियम हैं।
दूसरे सत्र में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ दिनेश कुमार ने सिनॉप्सिस लेखन पर विस्तार से अपने विचारों को उल्लेखित किया। इन्होंने बताया कि शोध प्रारूप की बारीकियों पर नजर रखना आवश्यक है विशेष रूप से शोधप्रनाली को स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। हमें शोध प्रारूप तैयार करते समय रिसर्च डिजाइन को हमेशा सामने रखना होगा। सांख्यिकी का उपयुक्त उपयोग पर भी पैनी दृष्टि रखनी होगी। रेफरेंस को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित रखकर उसे सिनॉप्सिस में शामिल करना होगा।
प्रो डॉ एम आई रहमान कार्यशाला के निदेशक ने दोनों विषय विशेषज्ञ का विभाग में अभिनन्दन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।
कल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के डा अरमान आलम एवम् तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रो डॉ नेसार अहमद कार्यशाला में भाग ले रहे सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगे।