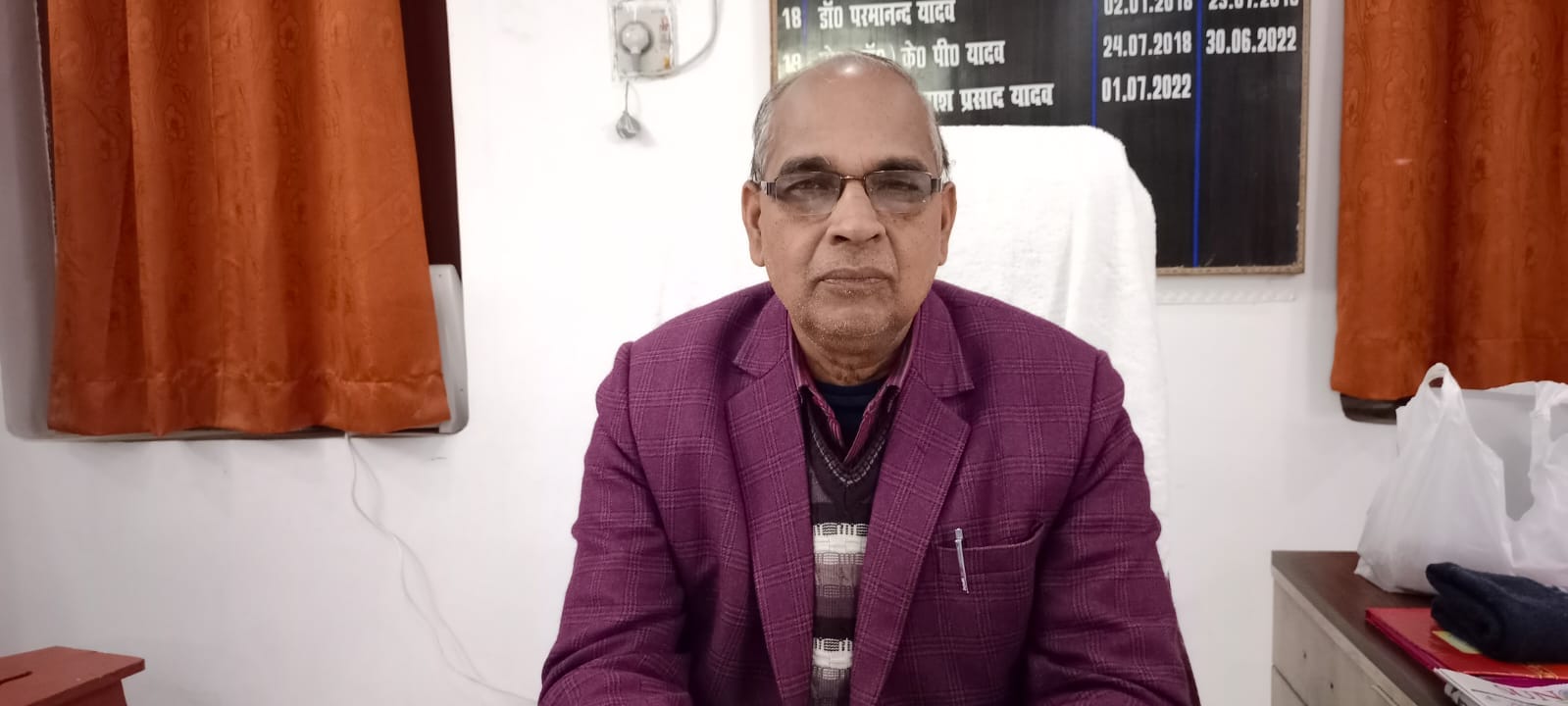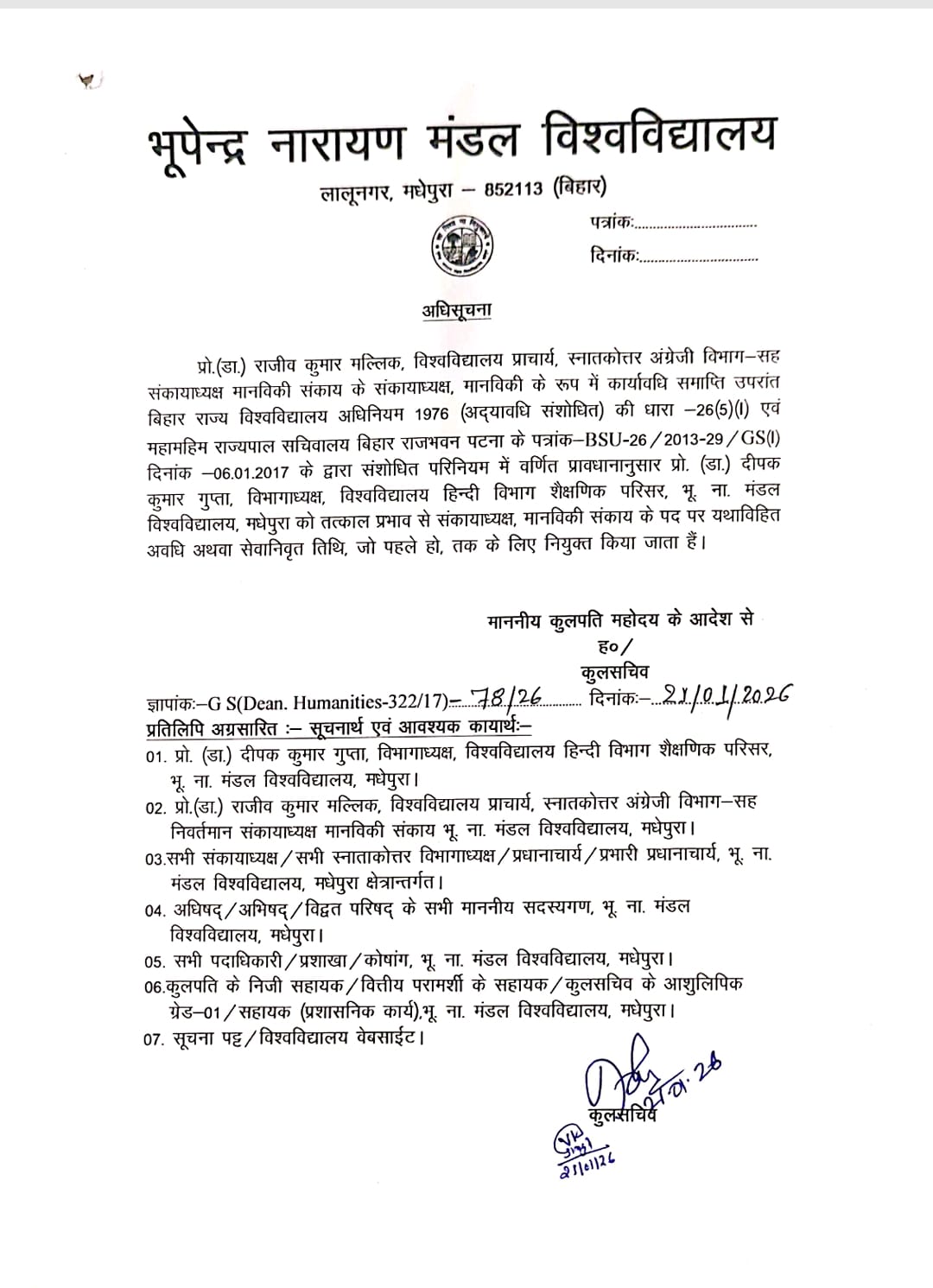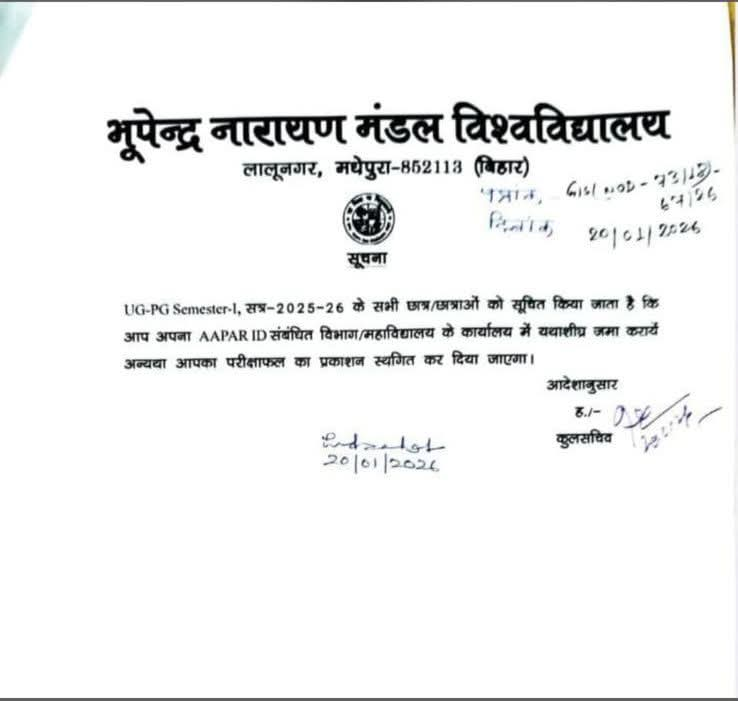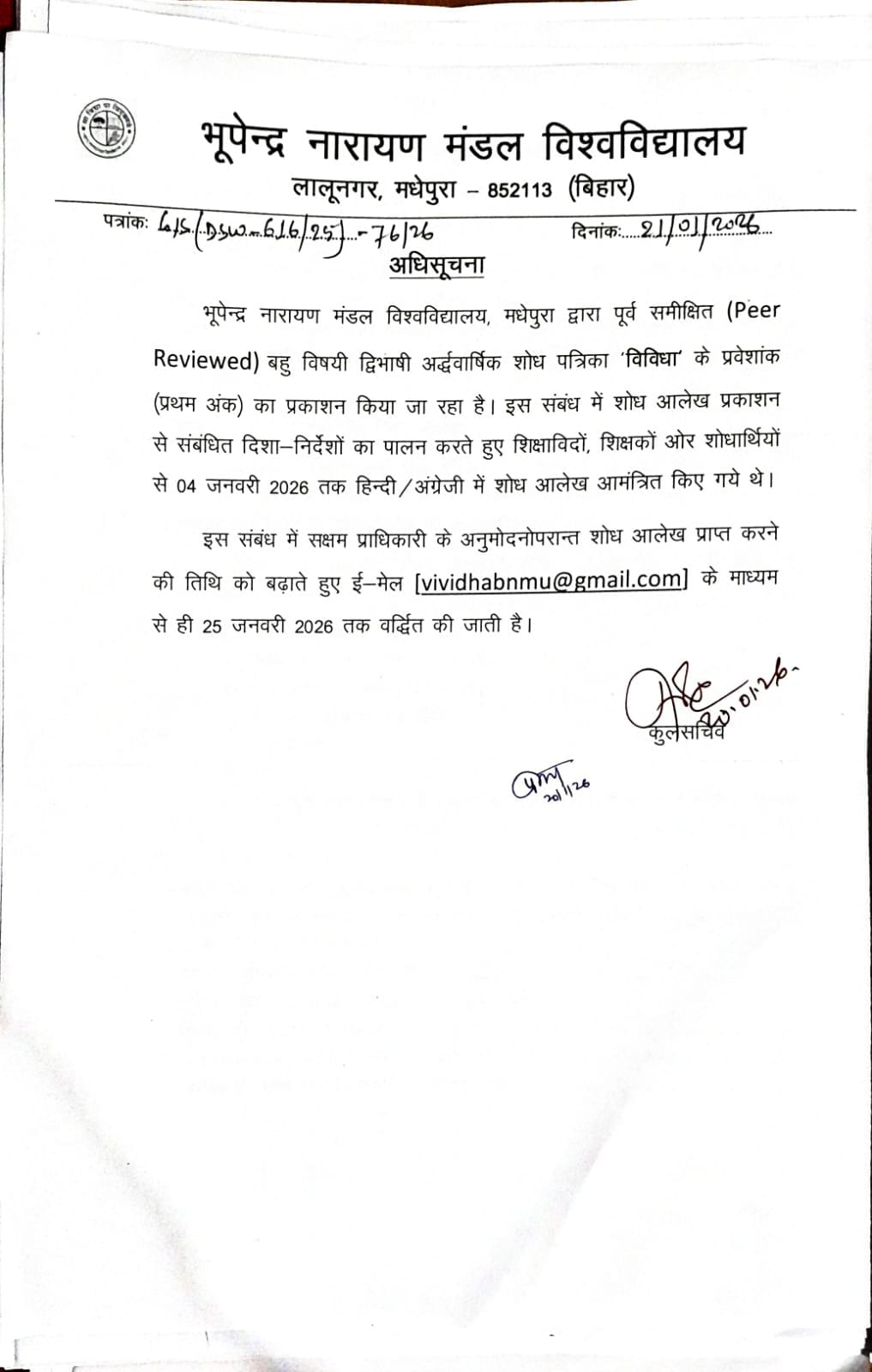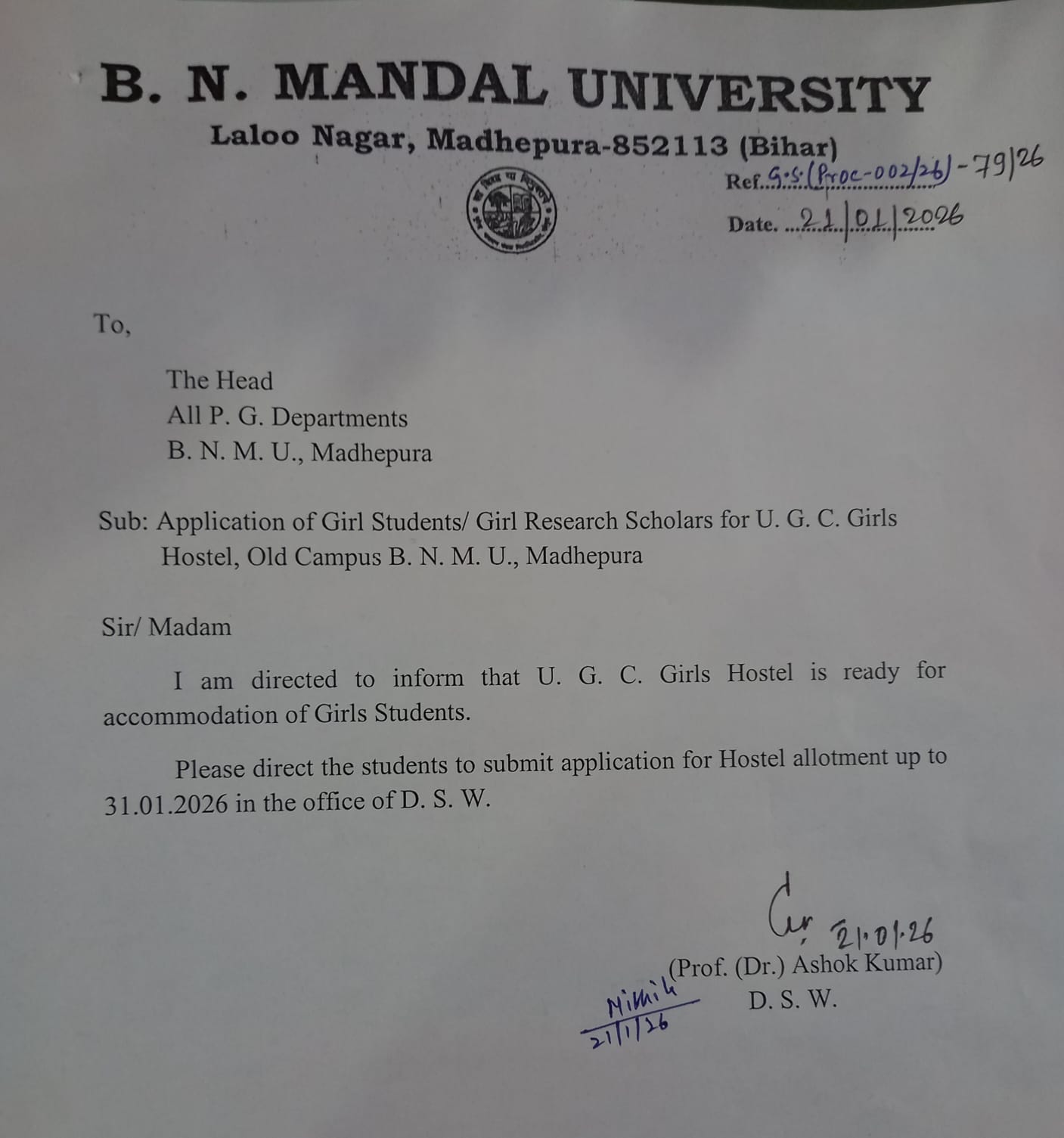क्या ‘दिवंगत आत्मा’ का प्रयोग उचित है?
श्री प्रभाकर मिश्र ने जानना चाहा है कि क्या किसी मृत व्यक्ति के लिए ‘दिवंगत आत्मा’ का प्रयोग सही है? लगभग ऐसा ही प्रश्न प्रो. गणेशानन्द झा के दोनों नातियों ने भी किया है। इन दोनों बच्चों ने जिज्ञासा रखी है कि आत्मा जब एक है, तब प्राणियों में अनेक कैसे हो जाती है?
सर्वप्रथम ‘दिवंगत आत्मा’ की व्याकरणिक विचिकित्सा करते हैं, फिर दार्शनिक विमर्श।
यहाँ ‘दिवंगत’ शब्द विशेषण है, जबकि ‘आत्मा’ विशेष्य। दिवम-स्वर्गम् गतः दिवंगतः, अर्थात् स्वर्ग गया (हुआ) अथवा जो स्वर्ग चला गया। इसीलिए, इन्द्र को ‘दिवस्पति’ भी कहते हैं।
सतत गमन के अर्थ में प्रयुक्त परस्मैपद धातु ‘अत्’ (अत् सातत्यगमने: अ.-1/31) में ‘मनिण्’ प्रत्यय के योग से ‘आत्मन्’ शब्द बनता है, जो कर्त्ताकारक एकवचन में ‘आत्मा’ का रूप ग्रहण कर लेता है; यथा – आत्मा (एकवचन)-आत्मानौ (द्विवचन)-आत्मानः (बहुवचन)। संस्कृत में आत्मा शब्द पुलिंग है, जबकि हिन्दी में स्त्रीलिंग। किन्तु, हिन्दी में लिखित दर्शन की लगभग सारी पुस्तकों में ‘आत्मा’ का प्रयोग पुलिंग में हुआ है। जो हो, यहाँ ‘सातत्य-गमन’ का प्रयोग आत्मा की सतत गतिशीलता या चलायमानता के अर्थ में हुआ है। दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि आत्मा कहीं सदा के लिए टिकती-ठहरती नहीं। दर्शन की भाषा में इसे स्थानान्तरण या लोकान्तरण कहते हैं, अर्थात् एक जगह से दूसरी जगह चला जाना।
मृड्. > मृ+त्युक् = मृत्यु का धात्वर्थ भी शरीर/प्राण का परित्याग होता है। प्रश्न है, शरीर/प्राण का परित्याग कौन करता है? इसका एकमात्र उत्तर होगा- आत्मा। गीता के अनुसार, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नये शरीर को उसीतरह धारण कर लेती है, जिसतरह मनुष्य पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेता है। यही आत्मा की गतिशीलता/चलायमानता अथवा अविनश्वरता है।
जब आत्मा अजर-अमर है, तब उसके लिए ‘मृत’ (मृतात्मा) अथवा ‘दिवंगत’ विशेषण का प्रयोग कैसे युक्तिसंगत होगा? मेरे फेसबुक-मित्र प्रभाकर मिश्र जी की यही मुख्य चिन्ता है।
चलिए, इसे तनिक विस्तार से समझाता हूँ।
उपनिषदों में आत्मा दो प्रकार की मानी गयी है- (1) वैयक्तिक आत्मा, अर्थात् जीवात्मा और (2) परमात्मा (ब्रह्म)। वैयक्तिक आत्मा/जीवात्मा कर्मबन्धन के कारण जन्म-मृत्यु के चक्कर में पड़कर दुख भोगती है। इससे मुक्ति के लिए उसे परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करना पड़ता है। वैशेषिक दर्शन (कणाद) भी आत्मा के दो भेद मानता है- जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अनित्य (नाशवान) है तथा शरीर-भेद से अनंत भी। परमात्मा नित्य और एक है। जीवात्मा के चौदह गुण होते हैं। इनमें पाँच सामान्य (संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग तथा विभाग)होते हैं, जबकि नौ (बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना, धर्म तथा अधर्म) विशेष गुण। जीवात्मा के बंधनमुक्त हो जाने पर ये विशेष गुण भी लुप्त हो जाते हैं। रह जाते हैं सिर्फ सामान्य गुण।
कणाद का वैशेषिक दर्शन आत्मा को असाधारण गुण चैतन्य से युक्त द्रव्य मानता है। प्राण-अपान नामक प्रयत्नों, उन्मेष-निमेष नामक कार्यों,
इस शरीर रूपी घर का अधिष्ठाता, मन सहित सभी इन्द्रियों का स्वामी तथा सुख-दुख, इच्छा-द्वेष इत्यादि मनोभावों की सूचक आत्मा है। यही कारण है कि वैशेषिक को अनेकान्तवादी दर्शन भी कहा जाता है।
जीवात्मा को अन्यत्र शरीरस्थ आत्मा भी कहा गया है। यह परमात्मा से भिन्न है। आत्मा की दो स्थितियाँ बताई गई हैं- अनुभवगम्य और वास्तविक। अनुभवगम्य (जीवात्मा) के तीन लक्षण माने गये हैं- (1) शारीरिक (2) मानसिक तथा (3) नैतिक।
आत्मा के शारीरिक लक्षण के अनुसार जीव जब संसार में प्रवेश करता है, तब उसे तीन प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है- स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर। स्थूल शरीर माता-पिता से प्राप्त होता है, जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर नामक पाँच तत्त्वों से बना होता है। यह अन्न द्वारा पुष्ट होने के कारण ‘अन्नमय कोष’ कहलाता है।
‘सूक्ष्म शरीर’ का दूसरा नाम ‘लिंग शरीर’ है; क्योंकि यह एक चिह्न के रूप में काम करता है। हम इसे बाहरी इन्द्रियों से नहीं देख सकते। जीवात्मा का यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच प्राणों, अर्थात् कुल सत्रह तत्त्वों से निर्मित होता है। जीवात्मा मृत्यु की स्थिति में स्थूल शरीर का तो त्याग करती है, किन्तु सूक्ष्म शरीर का नहीं। वह इसे अपने साथ लेकर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। पूर्व जन्म के संस्कारों, आचार-विचार, इच्छा-कर्म इत्यादि के अनुरूप उसे अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है।
‘कारण शरीर’ जीवात्मा का मूलाधार है। इसी से उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। ‘कारण शरीर’ गहरी निद्रावस्था की आनंदमयी अनुभूति की चरमावस्था है। जीवात्मा जब इन तीनों शरीरों से छुटकारा पा जाती है, तब विशुद्धावस्था में पहुँच जाती है।
जीवात्मा के मानसिक लक्षण भी तीन होते हैं; जैसे – ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इच्छा, क्रिया और ज्ञान जीवात्मा की शारीरिक शर्त्तें हैं।
आत्मा की चेतना चार प्रकार की होती है- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। जाग्रतावस्था में वह देशकाल की द्रष्टा है। स्वप्नावस्था में वह ‘तेजस’ कहलाती है। तेजस का अर्थ होता है- सूक्ष्म शरीर की अचेतन अवस्था की इच्छा और संस्कारों का प्रभाव। स्वप्नावस्था में वह प्रज्ञा कहलाती है। तुरीयावस्था विशुद्धावस्था का नाम है।
कायिक, मानसिक तथा वाचिक ये आत्मा के तीन गुण हैं। तीनों त्रिगुण से युक्त होते हैं।
नित्य, मुक्त और बद्ध। सदैव मुक्तावस्था में रहने वाली जीवात्मा नित्य कहलाती है। देवर्षि नारद, भक्त ध्रुव, प्रह्लाद प्रभृति इसके उदाहरण हैं। एकबार बंधन में पड़ जाने के बाद शीघ्र ही मुक्त हो जानेवाली आत्मा मुक्त कहलाती है; जैसे – राजर्षि जनक, महर्षि वसिष्ठ प्रभृति। सांसारिक बंधनों (वासना, इच्छा, राग-द्वेष इत्यादि) में बँधी आत्मा ‘बद्ध’ कहलाती है। फलस्वरूप, वह जन्म-मरण के चक्र से छूट नहीं पाती।
मुण्डकोपनिषद् ने इसे एक रूपक के सहारे समझाया है। मनुष्य-शरीर एक वृक्ष है, जिसमें हृदय रूपी घोसला स्थित है। उसमें जीवात्मा और परमात्मा नामक दो पक्षी परस्पर सखा-भाव से रहते हैं। जीवात्मा-पक्षी तो उस शरीर रूपी वृक्ष में फले सुख-दुख आदि फलों को स्वाद लेकर खाता रहता है, किन्तु परमात्मा-पक्षी मात्र उसे खाते हुए देखता रहता है। आशय यह कि जीवन संसार की विविध आसक्तियों में लिप्त है, जबकि परमात्मा पूरी तरह निर्लिप्त-निर्विकार। देखिए-
‘‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया/ समानं वृक्षं परिष्वजाते।/ तयोरन्यः पिपप्लं स्वाद्वात्त्यनषश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।।1।।
लगभग सभी विचारधाराओं ने आत्मा का अपनी-अपनी तरह से विवेचन किया है। विस्तार में नहीं जाकर यहाँ मैं न्याय दर्शन (गौतम), सांख्य (कपिल) तथा अद्वैत वेदान्त (शंकराचार्य) के आत्म-चिन्तन को आपके समक्ष रखना चाहूँगा।
न्याय दर्शन अत्यन्त प्राचीन दर्शन होने के बावजूद तर्कवादी दर्शन है। तर्कशास्त्र का अस्तित्व बौद्ध दर्शन से पहले का है। इसका पुराना नाम ‘आन्वीक्षकी’ है, जिसका अर्थ होता है- प्रत्यक्ष तथा आगम के द्वारा प्राप्त ज्ञान (प्रत्यक्ष) तथा शब्द के द्वारा उपलब्ध विषय का अवलोकन। न्याय का अर्थ ही होता है, जिसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध कर किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुँचा जा सके।
न्याय दर्शन के अनुसार, आत्मा स्पर्श आदि गुणों से रहित चैतन्य (ज्ञान) का अमूर्त्त आश्रय है, अर्थात् निराकार है, देशकाल के बंधनों से मुक्त है, अनादि और अनंत है।
ससीम शरीर के साथ उसका संयोग पूर्वजन्म के कर्माें का फल है, अर्थात् शरीर का भोगायतन (आत्मनो भोगायतनं शरीरम्) है।
न्याय आत्मा के दो भेद मानता है- जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अनेक है, अर्थात् शरीर की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान इसके छह गुण हैं। जबतक जीवात्मा शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती, तबतक ये सारे गुण जीवात्मा में बने रहते हैं। मोक्ष के बाद जीवात्मा शांत और निर्विकार हो जाती है। दूसरी ओर परम आत्मा एक है और सदैव निर्विकार-निर्गुण भाव से विराजती है। न्याय दर्शन आत्मा को सारथी और शरीर को रथ मानता है। इसके विपरीत ‘कठोपनिषद्’ में ‘आत्मा’ को रथी बताया गया है, जबकि ‘बुद्धि’ को सारथी। देखिए तृतीय वल्ली का तीसरा छन्द – ‘‘आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु/ बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।।3।।
गीता यही बात पहले ही कह चुकी है।
सांख्य के प्रवर्त्तक महर्षि कपिल उपनिषद्-काल के विचारक माने जाते हैं। उन्होंने आत्मा को ‘पुरुष’ नाम दिया है, जो प्रकृति के सहयोग से सृष्टि की रचना करता है। वह प्राणवान है। वही ज्ञान की ग्रहीता और चैतन्यस्वरूप है।
पुरुष या आत्मा एक है या अनेक, इसे लेकर दार्शनिकों में मतभेद है। वेदान्ती एक मानते हैं तो सांख्य के अनुयायी अनेक। उनका तर्क है कि यदि आत्मा एक है तो शरीर के नष्ट हो जाने पर एक ही साथ सभी शरीरों को नष्ट हो जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, एक शरीर के जन्म लेने पर एक ही साथ सभी शरीरों को जन्म लेना चाहिए था। एक शरीरधारी व्यक्ति के लूला-लंगड़ा-अंधा हो जाने पर सभी व्यक्तियों को हो जाना चाहिए था। पर, ऐसा देखा नहीं गया। इससे साबित होता है कि जिसतरह शरीर अनेक हैं, उसी तरह आत्माएँ भी अनेक हैं।
छान्दोग्य उपनिषद् (अयमात्मा ब्रह्म = यह आत्मा ही ब्रह्म है।) तथा वृहदारण्यकोपनिषद्’ (य आत्मनि तिष्ठन्) की तरह अद्वैत वेदान्त भी कहता है- जीवो ब्रह्मैव नापरः (शंकराचार्य), अर्थात् जीव ही ब्रह्म(परमात्मा) है। दोनों में कोई भेद नहीं; वह आनंदस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, सत्य है, नित्य है, शुद्ध-बुद्ध है, मुक्त है। तीनों अवस्थाओं में उसकी अवस्थिति एक-सी है।
जीवात्मा ही परमात्मा है, यही बात गीता में श्रीकृष्ण के मुख से निकली है- ‘‘अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः”।
(हे निद्राजयी अर्जुन!सारे जीवों के भीतर आत्मा के रूप में मैं ही विराजता हूँ।) अतः, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अन्तर नहीं।
इसी विमर्श के आलोक में अपने जिज्ञासु मित्रों की जिज्ञासाओं के शमन की चेष्टा कर रहा हूँ।
‘दिवंगत आत्मा’ में जो ‘आत्मा’ प्रयुक्त हुई है, वह जीवात्मा/शरीरस्थ आत्मा है। शरीर धारण करने के परिणामस्वरूप उसे तमाम शारीरिक या सांसारिक दुख-सुख, शुभ-अशुभ भोगने पड़ते हैं। सांसारिक बंधन से मुक्ति के लिए उसमें छटपटाहट भी होती है। उसे नारकीय कष्ट से भय लगता है तो स्वर्गिक सुख के प्रति दुर्निवार आकर्षण भी। इसके लिए उसे सत्कर्म करने पड़ते हैं। जन्म-मरण के चक्र में न फँसना पड़े, इसके लिए तदनुरूप आचरण करती है। ऐसा करके वह परमात्मा के सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य-सुख की प्राप्ति कर सकती है। जब ऐसी आत्मा अथवा मनुष्य शरीर/प्राण त्यागती है, तब उसके लिए ‘दिवंगत आत्मा’ का प्रयोग अनुचित नहीं कहलाएगा। लेकिन, आश्चर्य तो तब होता है, जब पापी से पापी व्यक्ति (मृत्यु के बाद) के लिए भी ‘स्वर्गीय’ या ‘दिवंगत’ विशेषण का प्रयोग होता है। परंपरा भी यही है। किसी मृत पापी मनुष्य के लिए ‘नारकीय’/‘नरकीय’ अथवा ‘नरकंगत’ विशेषण का प्रयोग होते नहीं देखा है। रावण, कंस, अजामिल- जैसे पापात्माओं के लिए भी नहीं; क्योंकि पहले दोनों जीव भगवान के हाथों मारे गये तो अजामिल ने अंतिम समय में ‘नारायण’ का नामोच्चार कर अपने लिए स्वर्ग सुरक्षित करा लिया। इसीलिए, स्वर्गंगत/दिवंगत कहलाए।
स्व. प्रो. गणेशानन्द झा के दौहित्र-द्वय के प्रश्न का उत्तर वैशेषिक, न्याय और सांख्य के विमर्श में ही निहित है। शरीर-भेद-आत्मा की अनेकता है।
आशा करता हूँ, उपरिनिर्दिष्ट जिज्ञासु मित्रों के साथ-साथ अन्य मित्रों की सम्बद्ध जिज्ञासाओं का भी यथासंभव शमन हुआ होगा।
फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते!
# प्रो. (डाॅ.) बहादुर मिश्र, पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
3 जुलाई 2020
(बीएनएमयू संवाद के लिए आपकी रचनाएं एवं विचार सादर आमंत्रित हैं। आप हमें अपना आलेख, कहानी, कविताएं आदि भेज सकते हैं।
संपर्क वाट्सएप -9934629245)